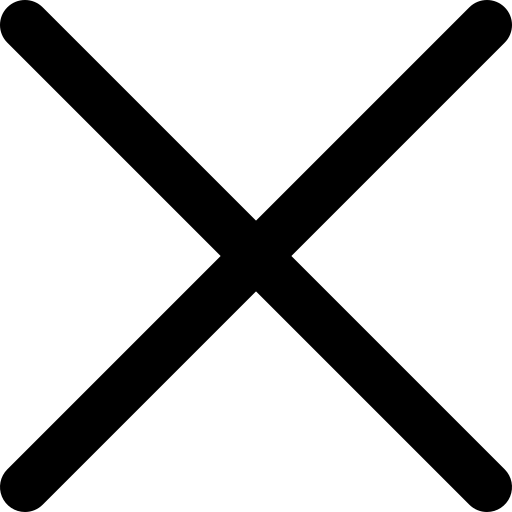नई दिल्ली
निजामुद्दीन बस्ती की अन्यथा चहल-पहल वाली गलियाँ वसंत की दोपहर में शांत होती हैं. कभी राष्ट्रीय राजधानी के बीचों-बीच झुग्गी-झोपड़ियों का इलाका हुआ करता था, लेकिन अब इस बस्ती में ऐसी इमारतें हैं जो यहाँ के कुछ स्मारकों से भी ऊँची दिखाई देती हैं. धूल भरे रास्तों और गंदी गलियों से परे, निजामुद्दीन की क्षितिज रेखा पर पवित्र महीने के लिए परी रोशनी से सजे स्मारकों के गुंबद हैं और पृष्ठभूमि में हरे-भरे पेड़ हैं. 25वर्षीय इतिहास प्रेमी शुमायला कहती हैं, "मैं यहाँ पैदा हुई हूँ; मैं अपने चारों ओर इन स्मारकों को देखते हुए बड़ी हुई हूँ," जिनके लिए सफ़ेद संगमरमर के स्मारक और पिएट्रा ड्यूरा अलंकरण एक आम दृश्य थे. "मैंने उन्हें अपने घर की छत से देखा." तीन या चार साल की उम्र में, वह निजामुद्दीन की भव्य कब्रों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई, जब तक कि 10साल की उम्र में उसे एहसास नहीं हुआ कि कब्रों के साथ रहना बहुत आम बात नहीं है - निजामुद्दीन खास है! शुमायला ने कहा, "मुझे इतिहास से प्यार है. मेरा बचपन इतिहास की खोज में बहुत अच्छा बीता.
हम इन कब्रों में लुका-छिपी खेलते थे. यहाँ के स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं, लेकिन उनमें से सभी में प्रवेश के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं होती है." मैत्री कॉलेज से स्नातक शुमायला ने लेडी श्री राम कॉलेज से इतिहास में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा निज़ामुद्दीन हेरिटेज क्षेत्र में एक टूर गाइड के रूप में काम करती है और शिक्षा के क्षेत्र में वापस लौटने का इरादा रखती है. शुमायला की आँखों में सितारे हैं, जबकि 43वर्षीय सीमा अली ने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है कि वह अपनी बेटियों को अपनी ज़िंदगी खुलकर जीने का मौका दे सकें. सीमा कहती हैं, "पहले समाज बहुत रूढ़िवादी था; अब इसमें काफी बदलाव आया है." उन्होंने बताया कि जब वह बड़ी हो रही थीं, तो लड़कियों को बाहर निकलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी. "लेकिन अब हम जानते हैं," उन्होंने कहा, "बच्चे इलाके को अच्छी तरह से जानते हैं और उनके पास काम भी है.
"परिवर्तन होने के कारण, सीमा का स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के इस दिन तक का सफ़र आसान नहीं था. जब उसने बाहर जाकर काम करने का फैसला किया, तो उसकी इच्छा अनिच्छा से पूरी हुई.
सीमा को अपने पति का समर्थन तभी मिला जब उसकी 8,000से 10,000रुपये की मासिक आय ने उसे आश्वस्त किया कि वह काम करने के योग्य है.
"वे यह पसंद नहीं करते कि महिलाएँ घर से बाहर निकलें और काम करें. लेकिन मेरे पति ने देखा कि हम सुरक्षित हैं और घर से बहुत दूर नहीं हैं. अब वह मुझे उन जगहों पर छोड़ देता है जहाँ प्रदर्शनी होती है, भले ही वे बहुत दूर हों. मैंने अपनी कमाई से उसे एक स्कूटी उपहार में दी," उसने गर्व से कहा.
सीमा एक कारीगर के रूप में काम करती है और क्रॉचेट शिल्प बनाने और बेचने में बड़े पैमाने पर शामिल है. यह एक ऐसा शिल्प है जो पारंपरिक रूप से उसे सौंपा गया था, लेकिन उसने, कई महिलाओं की तरह, इसे अपने घर तक ही सीमित रखा. अब, वह एक सामूहिक की प्रमुख सदस्य है.
सूती धागे से एक फूल बुनने में उसे एक घंटा लगता है. कई बार वह अपना काम घर भी ले जाती है. कच्चा माल मुहैया कराया जाता है और शिल्प बनाने के लिए उसे सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है.
सीमा इसे सख्त शब्दों में नौकरी नहीं कहती, लेकिन वह अपने लाभकारी काम से खुश है और अपने घर और परिवार पर पूरा ध्यान देने, अपनी माँ और पत्नी के कर्तव्यों का पालन करने और घर से बाहर काम करने के लिए किसी को भी उसके खिलाफ बोलने नहीं देने की जिम्मेदारी खुद पर लेती है.
एक महिला के घर-आधारित कर्तव्यों से यह विविधता सीम्स के घर पर भी दिखाई देती है:
"पहले, मैं अपने पति की आय पर निर्भर थी," लेकिन अब वह घर में सक्रिय रूप से आर्थिक रूप से योगदान देती है. उसने एक बेशकीमती निजी संपत्ति दिखाई. "मैंने खुद को ये उपहार में दिए हैं," उसने खुशी से कहा, अपनी सोने की बालियाँ दिखाते हुए जो उसने कमाई शुरू करने के एक साल बाद खरीदी थीं.
सीमा एक दशक से अधिक समय से ईशा-ए-नूर के साथ काम कर रही है, जो आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर (AKTC) के तहत एक पहल है, जिसका उद्देश्य शिल्प-आधारित कौशल के माध्यम से शामिल महिलाओं को बेहतर और सम्मानजनक आजीविका के अवसर प्रदान करना है. AKTC एक स्वयं सहायता समूह सैर-ए-निजामुद्दीन भी चलाता है, जिसमें आस-पास के युवा शामिल हैं, जो उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं. AKTC की कार्यक्रम अधिकारी रांता साहनी ने ANI को बताया कि 2009 में निजामुद्दीन बस्ती का एक आधारभूत सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें पता चला था कि केवल नौ प्रतिशत महिलाएँ अपने घरों से बाहर काम करती हैं और आस-पास के इलाकों में घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती हैं. उन्होंने कहा, "शिक्षा की कमी है, लेकिन समुदाय अपने हाथों से चीज़ें बनाने की ओर झुका हुआ है - ये भी उनका पारंपरिक कौशल है." इससे उनके लिए सम्मानजनक आय उत्पन्न करने का अवसर पैदा हुआ.
साहनी ने कहा, "कुछ आगे आने वाली महिलाओं ने अन्य महिलाओं को बाहर आने के लिए राजी करने में मदद की." पैसे कमाना और घर में योगदान देना उनके लिए लगे रहने की सबसे बड़ी प्रेरणा थी. उन्होंने कहा, "उन्हें अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए किसी से पैसे नहीं मांगने पड़े." समाज के इस तबके में श्रम की गरिमा, जहाँ महिलाएँ बमुश्किल साक्षर हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी यह मानने के लिए तैयार की जाती हैं कि दुनिया घर और परिवार से शुरू होती है और खत्म होती है, उनके लिए सशक्तिकरण का क्या मतलब है? कि उनके पास पर्याप्त पैसा है और वे परिवार पर निर्भर नहीं हैं, जबकि वे अभी भी सब कुछ संभाल रही हैं; साहनी ने कहा, "मुझे घूमने-फिरने की आज़ादी है, इसके लिए साधन और अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं."
32वर्षीय सैबा के लिए, यह वह सशक्तिकरण है जिसने उन्हें पिछले पाँच वर्षों से एक निजी स्कूल में अपनी बेटी की शिक्षा का खर्च वहन करने की अनुमति दी है. "अगर यह [कमाई का अवसर] नहीं होता, तो मैं अपने बच्चे को एक निजी स्कूल में भेजने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी," उन्होंने कहा. तीन बच्चों की माँ पीक सीज़न में 15,000से 20,000रुपये प्रति माह कमाती हैं. सैबा खाना बनाती हैं, बिल बनाती हैं और प्राप्त ऑर्डर की तैयारी की देखरेख करती हैं, इसके अलावा दिल्ली और यहाँ तक कि अन्य प्रमुख शहरों में विभिन्न स्थानों पर आयोजित खानपान के आयोजनों में एक प्रमुख व्यक्ति भी हैं. AKTC के तहत एक और संपन्न पहल, ज़ायका-ए-निज़ामुद्दीन, एक महिला उद्यम है जो 700साल पुराने पाक इतिहास की विशेषताओं को पूरा करता है जो निज़ामुद्दीन व्यंजन और स्वस्थ घर का बना नाश्ता बनाती हैं. ज़ायका-ए-निज़ामुद्दीन की रसोई में अपने खाना पकाने के कौशल का मुद्रीकरण करने से लेकर विविधता लाने तक उद्यमशीलता के क्षेत्र में उनकी भूमिका के अलावा, उनकी यात्रा भी, निश्चित रूप से कठिन थी.
साइबा कहती हैं कि सबसे पहले एक करीबी पारिवारिक सदस्य ने आपत्ति जताई थी, जिन्होंने लंबे समय तक घर से उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठाया था और कहा था कि "मामूली आय" उनकी अनुपस्थिति को उचित नहीं ठहराती.
शुरुआत में, समुदाय के लोग बस्ती में बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए अपने घरों के लिए स्वस्थ नाश्ता बनाने में लगे हुए थे. उन्हें अपने घरों से बाहर जाकर ज़ायका-ए-निज़ामुद्दीन की रसोई के ज़रिए पड़ोस में बिक्री के लिए नाश्ता बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया. हालाँकि, यह व्यापार इतना सफल नहीं हुआ कि महिलाएँ लंबे समय तक अपने घरों से दूर रहें, और इससे मिलने वाला लाभ भी कुछ खास नहीं था.
साइबा की अधेड़ उम्र की सास को इस बात पर बहुत आपत्ति थी और वह इस बात से खुश नहीं थीं कि उनकी बहू 2012में सिर्फ़ 600-700रुपये महीना कमा रही थी. हालाँकि, उन्होंने घर की ज़िम्मेदारियों में बहुत कम मदद की.
लेकिन समूह की दूसरी महिलाओं की तरह साइबा ने भी हार नहीं मानी. धीरे-धीरे लाभ बढ़ने लगा, खानपान का व्यवसाय चल निकला और उन्हें प्रीमियम होटलों में आमंत्रित किया जाने लगा जहाँ उन्होंने अपने रसोइयों से सीखा.
इस रसोई की महिलाओं ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. परिवारों की अनिच्छा स्वीकृति में बदल गई.
अपने पेशेवर दायित्वों और परिवार के साथ तालमेल बिठाते हुए, साइबा अपने बच्चों के साथ समय बिताती हैं, अपनी शिफ्ट और घर के कामों के बीच के घंटों को ध्यान में रखते हुए. उन्हें क्या जुड़ा रखता है? "रसोई में होने का मज़ा. और कर्तव्य," उसने कहा.
एक मददगार हाथ
ए.के.टी.सी. के सी.ई.ओ. रतीश नंदा ने ए.एन.आई. को बताया कि कैसे उनके संगठन ने निज़ामुद्दीन बस्ती की महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में मदद की और स्मारकों के संरक्षण में भी योगदान दिया. "भारत सरकार ने हमें देश भर में 50साइटों का विकल्प दिया. ए.के.टी.सी. ने हुमायूं के मकबरे पर वापस जाने का विकल्प चुना - इससे पहले मकबरे के बगीचों के जीर्णोद्धार का काम किया था," उन्होंने कहा. "निज़ामुद्दीन में, हमने ज़रूरतों और आकांक्षाओं को समझने के लिए परियोजना की अवधि के दौरान सामुदायिक समूहों के साथ 5,000से ज़्यादा बैठकें की होंगी.
साथ ही, हर पाँच साल में, हमने अपने कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण किए हैं और हम कह सकते हैं कि हमने 99प्रतिशत निवासियों को सीधे तौर पर लाभान्वित किया है," उन्होंने आगे बताया.
नंदा ने कहा, "हम लगातार इसमें शामिल हैं और शिक्षा तथा स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए एमसीडी के साथ समझौते के नवीनीकरण की मांग की है." नंदा ने एएनआई से कहा, "कई कार्यक्रम पहले से ही आत्मनिर्भर बन चुके हैं, कुछ ने अपने उद्देश्य हासिल कर लिए हैं और इसलिए हमने कुछ व्यक्तिगत कार्यक्रम बंद कर दिए हैं." यदि अधिक संस्थाएं समान उद्देश्य वाले समुदायों से जुड़ना चाहती हैं, तो उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए? क्या सरकार का समर्थन अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है?
नंदा ने कहा, "महत्वपूर्ण रूप से, संस्थाओं को यह समझने की आवश्यकता है कि कोई शॉर्टकट नहीं है - समुदाय का विश्वास बनाने और समुदाय की जरूरतों को समझने में हजारों घंटे की बैठकें और कई महीने, यहां तक कि साल भी लग सकते हैं." यह बताते हुए कि एक अंतर-अनुशासनात्मक टीम उनकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण रही है, नंदा ने कहा: "दिल्ली नगर निगम और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ साझेदारी हमें बुनियादी ढांचे को लागू करने में सक्षम बनाती है", जिसमें स्मारकों का संरक्षण शामिल है, जिसने बदले में, यहां के स्थानीय निवासियों को अपनी आजीविका में सुधार करने में मदद की है. ज़ियाका-ए-निज़ामुद्दीन की विशाल रसोई में, मगरिब की अज़ान सुनाई दी है; सैबा अपनी सहकर्मी की देखरेख करती हैं, जब वह ऑर्डर के लिए कबाब तैयार करती हैं, जबकि दूसरी अपनी नमाज़ पढ़ती हैं. इफ़्तार का समय हो गया है, और महिलाओं को अपने परिवार के पास घर जाना है. क्या इस समय बहुत काम नहीं है? "मैं इस बीच चूल्हे पर कुछ रखूँगी और नमाज़ के लिए जाऊँगी," सैबा कहती हैं, जब वह घर वापस लौटती हैं, "मेरे बेटे ने कुछ फल काटे होंगे."