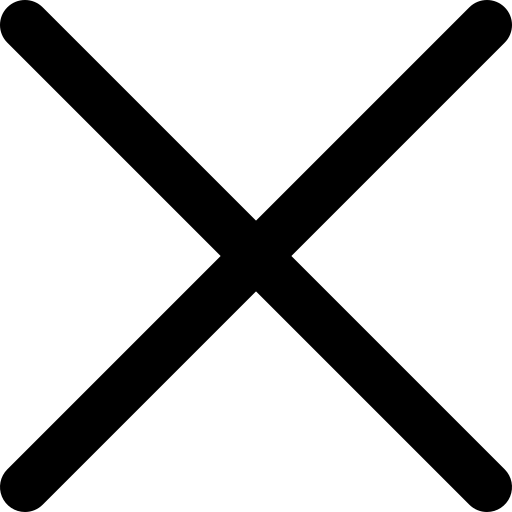राकेश चौरासिया / नई दिल्ली
भारत ईश्वर की लीलाओं की साक्षी धरा है. ईश्वर के पूर्णावतारों, अंशावतारों, ऋषियों, मुनियों, मनीषियों की श्रंखला में आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती अद्वितीय प्रकाश पुंज हुए, जिन्होंने वेदों को पुनर्स्थापित और पुनर्भाषित कर आमजन के लिए सुगम बनाया.
खास बात यह है कि स्वामी दयानंद न केवल वृहद हिंदू समाज के लिए आदरणीय रहे, बल्कि किंचित मुस्लिम आलिमों द्वारा भी सराहे गए. ऐसे ही एक प्रगतिशील मुस्लिम विचारक एवं शिक्षाविद् तथा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (तत्कालीन मुहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज) के संस्थापक सर सैयद अहमद ने स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों का मर्म समझने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया था.
भारत की हिंदू-मुस्लिम चेतना को जागृत करने वाले दो कर्मयोगी, स्वामी दयानंद सरस्वती और सर सैयद अहमद एक-दूसरे के समकालीन थे और वे एक-दूसरे का सम्मान भी करते थे. यद्यपि इस्लाम और कुरआन के बारे में स्वामी दयानंद के विचार भिन्न थे.
तथापि स्वामी दयानन्द की मृत्यु पर लिखे संस्थान राजपत्र के ‘संपादकीय’ में सर सैयद अहमद ने भारत की भलाई में स्वामी दयानंद सरस्वती के सराहनीय योगदान के लिए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी. सर सैयद अहमद का स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में एक उद्धरण बहुत मकबूल हुआ, ‘‘स्वामी जी ऐसे विद्वान और श्रेष्ठ व्यक्ति थे, जिनका अन्य मतावलम्बी भी सम्मान करते थे.’’
यह सर्वव्यापक है कि स्वामी दयांनद सरस्वती ने सनातन वैदिक हिंदू धर्म की कुरीतियों और रूढ़ियों पर प्रबल प्रहार किया और समाज को जागृत करने का कार्य किया. स्वामी दयानंद सरस्वती जन सामान्य को वेदोन्मुख करने के लिए अलख जगाए हुए थे, लेकिन लोग तत्व दर्शन के स्थान पर कर्मकांडों में अत्यधिक व्यस्त थे.
कुछ स्थानों पर स्वामी दयानंद सरस्वती की चर्चाओं और दर्शन को सम्मान भी मिला, लेकिन प्रयागराज और वाराणसी जैसे सनातन धर्म के प्रमुख केंद्रों में उनकी बातों पर लोग ध्यान नहीं दे रहे थे. बनारस में वेद ज्ञान के प्रसार के लिए तो उन्होंनेतब नौ बार दौरा किया था.
ऐसे में, सर सैयद अहमद ने स्वामी दयानंद सरस्वती को अपने घर आमंत्रित किया और स्वामी दयानंद से वेद मंत्र सुने और उनका सार जाना. दरअसल, स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा जय किशनदास के मध्य मधुर संबंध थे.
राजा जय किशनदास, स्वामी दयानंद सरस्वती के अभियान से प्रभावित थे और उनके प्रशंसक थे. जब भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी अलीगढ़ जाते थे, तो वे राजा जय किशनदास के निवास पर ही प्रवास करते थे. जब उनके आगमन का समाचार मिलता था, तो सर सैयद अहमद उनसे मिलने राजा जय किशनदास जी के घर जरूर जाते थे.
सर सैयद अहमद खुले विचारों के व्यक्ति के थे और ज्ञान पिपासु थे. इसलिए उन्होंने सनातन धर्म के मूल वेदों को जानने की लालसा से स्वामी दयानंद सरस्वती को अपने घर बुलाया था. हालांकि तब मुस्लिम समाज ने सर सैयद अहमद के स्वामी दयानंद सरस्वती से वेद सुनने के कार्य पर ऐतराज उठाया था और इसे कुफ्र करार दिया था.
किंतु सही अर्थों में समाज की चिंता करने वाले इन दोनों ही महानुभावों को समाज के कुछ खित्तों के अनर्गल प्रलापों की चिंता जरा भी न थी. न सर सैयद अहमद ने स्वामी दयानंद सरस्वती से वेद सुनने में हिचक दिखाई और न स्वामी दयानंद सरस्वती ने उन्हें वेद भाष्य प्रदान करने में संशय प्रदर्शित किया.
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहासकार डॉ. राहत अबरार बताते हैं कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती को अपने अभियान में सफलता नहीं मिली, तो सर सैयद अहमद ने उन्हें अपने घर पर बुलाया. वहां स्वामी जी ने सर सैयद अहमद और कुछ अन्य मुसलमानों को वेद मंत्र सुनाए. इसका राजा शिव प्रसाद ने विरोध भी किया था. किंतु, सर सैयद का मानना था कि हमें एक-दूसरे के धर्म के बारे में जानना चाहिए. ये संवाद से ही संभव है. संवाद के बिना एक-दूसरे को समझ पाना संभव नहीं हैं.
दयानंद सरस्वती जयंती कब है ? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ ? स्वामी दयानंद का जन्म कहां हुआ था ? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का धर्म क्या था?
भारत की पुण्य धरा पर गुजरात के टंकारा प्रांत में एक ब्राह्मण परिवार में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को वर्ष 1824 ईसवी में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था. मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनका नाम मूल शंकर रखा गया.
हमारे सनातनी कैलेंडर के अनुसार, 26 फरवरी को इस महामानव की जयंती होती है. शाश्वत सत्य के अन्वेषण हेतु एवं सत्य व शिव की प्राप्ति हेतु मूल शंकर वर्ष 1846 में 21 वर्ष की आयु में समृद्ध घर-परिवार, मोह ममता के बंधनों को त्याग कर संन्यासी जीवन की ओर बढ़ गए.
स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु का नाम क्या था?
स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1859 में गुरु विरजानंद जी से व्याकरण व योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की. भारत की उत्कृष्ट वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता की हजारों वर्षों की गरिमामयी विरासत मध्यकाल के तमसाच्छन्न युग में लुप्तप्राय हो गई थी.
स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है? दयानंद सरस्वती क्यों प्रसिद्ध है? दयानंद सरस्वती ने हमारे समाज में कैसे योगदान दिया?
राजनीतिक परतंत्रता तथा पराधीनता के कारण विचलित भारतीय जनमानस को महर्षि दयानंद सरस्वती ने आत्मबोध आत्मगौरव स्वाभिमान एवं स्वाधीनता का मंत्र प्रदान किया. समकालीन विद्वानों ने इसीलिए उन्हें महर्षि की उपाधि भी प्रदान की.
महर्षि दयानंद के प्रादुर्भाव के समय भारत धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अतिजर्जर और छिन्न-भिन्न हो गया था. ऐसे विकट समय में जन्म लेकर महर्षि ने देश के आत्मगौरव के पुनरुत्थान का अभूतपूर्व कार्य किया.
लोक कल्याण के निमित्त अपने मोक्ष के आनंद को वरीयता न देकर जनजागरण करते हुए अंधविश्वासों का प्रखरता से खंडन किया. अज्ञान, अन्याय और अभाव से ग्रस्त लोगों का उद्धार करने हेतु वे जीवनपर्यंत संघर्ष करते रहे. महर्षि दयानंद ने सत्य की खोज के लिए अपने वैभवसंपन्न परिवार का त्याग किया.
दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना कहां हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज का इतिहास क्या है?
1875 में स्वामी दयानंद ने बंबई (अब मुंबई) में आर्य समाज की स्थापना की. उन्होंने वेदों को समस्त ज्ञान एवं धर्म के मूल स्रोत और प्रमाण ग्रंथ के रूप में स्थापित किया. अनेक प्रचलित मिथ्या धारणाओं को तोड़ा और अनुचित पुरातन परंपराओं का खंडन किया.
उस अंधकार के युग में महर्षि दयानंद ने सर्वप्रथम उद्घोष किया कि, च्वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है. वेद का पढना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है.् संपूर्ण भारतीय जनमानस को उन्होंने वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया. वेद के प्रति यह दृष्टि ही स्वामी दयानंद की विलक्षणता है. महर्षि दयानंद ने मनुष्य मात्र के लिए वेदों के अध्ययन के द्वार खोले थे, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त किया.
दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज को सुधारने का प्रयास कैसे किया? स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार क्या थे? दयानंद सरस्वती ने हमारे समाज में कैसे योगदान दिया? स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया?
उन्होंने मनुष्य को अपनी बुद्धि, विवेक शक्ति तथा चिंतन प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने राष्ट्रवाद के सभी प्रमुख सोपानों जैसे कि स्वदेश, स्वराच्य, स्वधर्म और स्वभाषा इन सभी के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया.
अंग्रेजों की दासता में आकंठ डूबे देश में राष्ट्र गौरव, स्वाभिमान व स्वराच्य की भावना से युक्त राष्ट्रवादी विचारों की शुरुआत करने तथा उपदेश, लेखों और अपने कृत्यों से निरंतर राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने के कारण महर्षि दयानंद आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के जनक थे. इसके लिए स्वामी दयानंद ने गुरुकुल पद्धति का विधान किया, ताकि राष्ट्र का प्रत्येक युवा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों से परिपूर्ण होकर भारतीय वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर हो. महर्षि दयानंद ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत जैसी अनेक सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जीवनपर्यंत संघर्ष किया. उन्होंने समाज में दलितों और शोषितों को समानता का अधिकार देकर सामाजिक एकता, समरसता व सद्भावना की नींव रखी.
महर्षि दयानंद के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा?
वेदों के स्वर्णिम चिंतन को महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, संस्कार विधि में प्रस्तुत किया. इनमें सत्यार्थ प्रकाश सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ.
स्वामी दयानंद सरस्वती नोट्स ? स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार ? दयानंद सरस्वती को एक महान मानवतावादी क्यों माना जाता है?
जाति प्रथा का विरोध
वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन
जाति प्रथा एवं अस्पृश्यता जैसी बुराइयों के प्रबल विरोधी होते हुए भी स्वामी दयानन्द वर्णाश्रम व्यवस्था को केवल सुधारना चाहते थे, समाप्त करना नहीं चाहते थे. वे केवल इतना चाहते थे कि जन्म के आधार पर वर्ण निश्चित नहीं किया जाना चाहिये, यह अनुचित है. वर्णों का आधार प्रारम्भ में भी जन्म नहीं कर्म ही था और कर्म हो होना भी चाहिये.
कर्म के साथ-साथ इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक एवं उचित है कि उस व्यक्ति के क्या गुण हैं तथा कैसी उसकी प्रकृति है. आर्य समाज ने वर्णाश्रम व्यवस्था के बन्धनों को बहुत कुछ ढीला अवश्य कर दिया.
स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे?
वैदिक धर्म तो स्वामी दयानन्द के श्वास में व्याप्त था परन्तु और शुद्ध वैदिक धर्म वह धर्म है जो वेदों के अनुसार था, अतः वैदिक धर्म को शुद्ध रखने के लिये वे उसमें घुस आई कुप्रथाओं का विरोध करते थे और उन्हें मिटाना चाहते थे.
वे बाल विवाह, दहेज-प्रथा जैसी प्रथाओं का विरोध करते थे और इसे अनुचित मानते थे कि विधवा विवाह की अनुमति न देकर महिलाओं पर बलात् वैधव्य के कष्ट को थोपा जाये. स्वामीजी ने ही सर्वप्रथम बाल विवाह के विरोध में विवाह की आयु निर्धारित करने की बात सुझाई थी.
उनका निश्चित मत था कि विवाह के लिये लड़कों की आयु 25 वर्ष और लड़कियों की आयु 16 वर्ष होनी चाहिये, क्योंकि इसी अवस्था में पहुँचने पर उनके शरीर के साथ-साथ बुद्धि और विवेक भी परिपक्व हो जाते हैं. विवेकपूर्वक चुने गये जीवन साथी के साथ जीवन सुखमय रहेगा तथा उचित आयु की सन्तान स्वस्थ और पुष्ट होगी. उन्होंने दहेज-प्रथा को समाज के लिये अभिशाप बताकर उसके उन्मूलन का प्रयत्न किया तथा विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन करके उनके जीवन को सुखी एवं यातनामुक्त बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाया.
शिक्षा सम्बन्धी विचार
शिक्षा के लिए गुरुकुल व्यवस्था-स्वामी दयानन्द समाज का सुधार करना चाहते थे. एक विद्वान की भाँति उन्होंने समाज में प्रचलित बुराइयों के कारण को ही समाप्त करना उचित समझा. समाज में पाखण्ड तथा मूर्ति-पूजा जैसी कुरीतियाँ थीं. इन सबका कारण अन्ध-विश्वास था जो अशिक्षा के कारण फैले हुए अज्ञान के कारण समाज में पनप रहा था.
अशिक्षा को समाप्त करने के लिये शिक्षा का प्रचार आवश्यक था. उसी के द्वारा हिन्दू समाज अज्ञान के अन्धकार से मुक्ति पा सकता था. स्वामी जी ने शिक्षा की ओर ध्यान दिया, परन्तु शिक्षा को उन्होंने उसके सम्पूर्ण व्यापक अर्थ में लिया. केवल पढ़ना-लिखना जानने को शिक्षा नहीं मान लिया.
वे मानते थे कि शिक्षा का अर्थ बौद्धिक विकास तो है ही, साथ ही शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति तथा इन्द्रिय साधना भी है. जिसे शिक्षा से ये तीनों गुण मिले हों वह ही वास्तव शिक्षित माना जा सकता है. शिक्षा से उनका तात्पर्य पाश्चात्य शिक्षा से नहीं था.
वे पाश्चात्य शिक्षा तथा शिक्षा पद्धति को भारतीयों के लिये घातक मानते थे. उनके विचार से भारतीयों के उत्थान के लिए गुरुकुल पद्धति ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धति थी और इसी का उन्होंने समर्थन तथा प्रचार किया. गुरुकुल में रहकर विद्यार्थी के दो मुख्य कर्त्तव्य होने चाहिएकृपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन तथा सम्पूर्ण विषयों का ज्ञानार्जन. यह सच्चरित्र गुरु द्वारा ही सम्भव था.
स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कैसे हुई ? स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब और कहां हुई ? दयानंद सरस्वती को जहर क्यों दिया गया था?
जोधपुर के महाराजा जसवन्त सिंह द्वितीय ने 1883 में स्वामी दयानंद को अपने महल में रहने के लिए आमंत्रित किया था. महाराजा दयानंद के शिष्य बनने और उनकी शिक्षाएं सीखने के लिए उत्सुक थे. स्वामी दयानंद सरस्वती अपने प्रवास के दौरान महाराजा के शौचालय में गए, तो उन्हें नन्हीं जान नाम की एक नाचने वाली लड़की मिली.
स्वामी दयानंद सरस्वती ने महाराजा से गणिका और सभी अनैतिक कार्यों को त्यागने और एक सच्चे आर्य (कुलीन) की तरह धर्म का पालन करने के लिए कहा. दयानंद की बात नन्हीं जान को नागवार गुजरी और उसने बदला लेने का फैसला कर लिया.
नन्ही जान ने 29 सितंबर 1883 को स्वामी दयानंद सरस्वती के रसोइये, जगन्नाथ को उनके रात के दूध में कांच के छोटे टुकड़े मिलाने के लिए रिश्वत दी. स्वामी दयानंद सरस्वती को सोने से पहले गिलास में दूध परोसा गया, जिसे उन्होंने तुरंत पी लिया और कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहे और असहनीय दर्द सहते रहे.
महाराजा ने तुरंत उनके लिए डॉक्टर की सेवाओं की व्यवस्था की. हालांकि, जब तक डॉक्टर पहुंचे, उनकी हालत खराब हो गई और उनमें बड़े रक्तस्रावी घाव हो गए थे. दयानंद की पीड़ा को देखकर, जगन्नाथ अपराध बोध से ग्रसित हो गया.
तब जगन्नाथ ने स्वामी दयानंद सरस्वती के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया. अपनी मृत्यु शय्या पर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उन्हें माफ कर दिया, और उन्हें पैसों से भराएक थैला दिया, और कहा कि महाराजा के आदमियों द्वारा पकड़े जाने और मारे जाने से पहले वे राज्य से भाग जाएं.
स्वामी दयानंद सरस्वती की पुण्य तिथि कब है?
बाद में, रेजीडेंसी की सलाह के अनुसार महाराजा ने उन्हें माउंट आबू भेजने की व्यवस्था की. हालाँकि, कुछ समय आबू में रहने के बाद, 26 अक्टूबर 1883 को उन्हें बेहतर चिकित्सा देखभाल के लिए अजमेर भेज दिया गया. उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही थी. 30 अक्टूबर 1883 को हिंदू महापर्व दीपावलि की सुबह मंत्रों का जाप करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती को देहावसान हो गया.