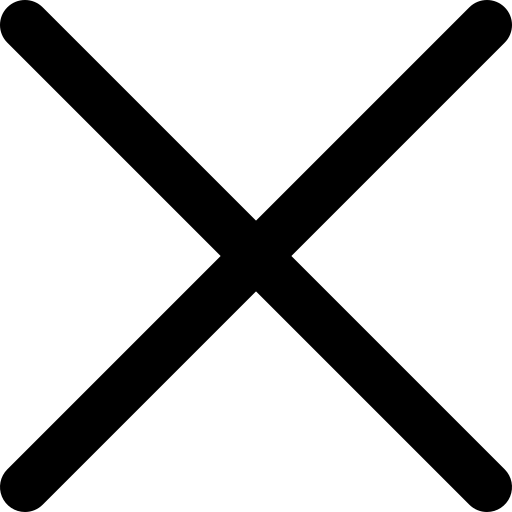ज़ाहिद ख़ान
'मैं अकेला ही चला था जानिब-ए-मंज़िल मगर/लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया' उर्दू अदब में ऐसे बहुत कम शे’र हैं, जो शायर की शिनाख़्त बन गए और आज भी सियासी, समाजी महफ़िलों और तमाम ऐसी बैठकों में कहावतों की तरह दोहराए जाते हैं. मजरूह सुल्तानपुरी गर अपनी ज़िन्दगी में इस शे’र के अलावा कुछ और नहीं लिखते, तब भी वे इस शे’र के बदौलत ही अदबी दुनिया में अलग से उनकी एक पहचान होती. ये बेश—क़ीमती शे’र है ही ऐसा, जो आज भी हज़ारों की भीड़ को आंदोलित, प्रेरित करने का काम करता है. इस शे’र को लिखे हुए एक लंबा अरसा गुज़र गया, मगर इस शे’र की तासीर ठंडी नही हुई.
उर्दू अदब में मजरूह सुल्तानपुरी का आगाज़ जिगर मुरादाबादी की शायरी की रिवायतों के साथ हुआ और आख़िरी वक़्त तक उन्होंने इसका दामन नहीं छोड़ा. मजरूह सुल्तानपुरी शुरू में तरक़्क़ीपसंद तहरीक की विचारधारा और सियासत से रज़ामंद नहीं थे.
इस विचारधारा से उनके कुछ इख़्तिलाफ़ थे, लेकिन बाद में वे इस तहरीक के सरगर्म हमसफ़र बन गए. उनका यक़ीन इस बात में पुख़्ता हो गया कि समाजी मक़सद के बिना कोई भी अज़ीम आर्ट पैदा नहीं हो सकती. एक बार उनका यह ख़याल बना, तो उनकी शायरी बा—मक़सद होती चली गई. मजरूह सुल्तानपुरी की शायरी का शुरुआती दौर, आज़ादी के आंदोलन का दौर था.
उस वक़्त जो भी इंक़लाबी मुशायरे होते, वे उनमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते. उनकी ग़ज़लों में तरन्नुम और सादगी का दिलकश मेल होता था. मजरूह की शुरू की ग़ज़लों को यदि देखें, तो उनमें एक बयानिया लहज़ा है, लेकिन जैसे-जैसे उनका तजुर्बा बढ़ा, उनकी ग़ज़लों की ज़बान और मौजूआत में नुमायां तब्दीली पैदा हुई और इशारियत (सांकेतिकता) और तहदारी (गहराई) में भी इज़ाफ़ा हुआ.
मजरूह सुल्तानपुरी उन शायरों में शामिल रहे, जिन्होंने ग़ज़ल की हमेशा तरफ़दारी की और इसे ही अपने जज़्बात के इज़हार का ज़रिया बनाया. ग़ज़ल के बारे में उनका नज़रिया था, 'मेरे लिए यही एक मोतबर ज़रिया है. ग़ज़ल की ख़ुसूसियत उसका ईजाज़-ओ-इख़्तिसार (संक्षिप्तता) और ज़ामइयत (संपूर्णता) व गहराई है. इस ऐतिबार से ये सब से बेहतर सिन्फ़ है.'
ग़ज़ल की जानिब मजरूह की ये बेबाकी और पक्षधरता आख़िर समय तक क़ायम रही. ग़ज़ल के विरोधियों से उन्होंने कभी हार नहीं मानी. अलबत्ता रिवायती ग़ज़ल के घिसे-पिटे मौज़ू और तर्ज़-ए-बयान को उन्होंने अपनी तरफ़ से बदलने की पूरी कोशिश की. जिसमें वे कामयाब भी हुए.

मजरूह की शायरी में रूमानियत और इंक़लाब का बेहतरीन संगम है. ऐसी ही उनकी एक ग़ज़ल के कुछ अश्आर इस तरह से हैं,'अब अहले-दर्द ये जीने का अहतिमाम करें/उसे भुला के गमे-ज़िंदगी का नाम करें./...ग़ुलाम रह चुके, तोड़ें ये बंदे-रुसवाई/ख़ुद अपने बाजू-ए-मेहनत का एहतिराम करें.'
मजरूह सुल्तानपुरी की इस बात से हमेशा नाइत्तेफ़ाक़ी रही, कि मौजूदा ज़माने के मसायल को शायराना रूप देने के लिए ग़ज़ल नामौज़ू है, बल्कि उनका तो इससे उलट यह साफ़ मानना था, 'कुछ ऐसी मंज़िलें हैं, जहां सिर्फ़ ग़ज़ल ही शायर का साथ दे सकती है.’’
कमोबेश यही बात क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार, मजरूह की एक मात्र शायरी की किताब ‘ग़ज़ल’ की प्रस्तावना में लिखते हुए कहते हैं, 'मजरूह का शुमार उन तरक़्क़ीपसंद शायरों में होता है, जो कम कहते हैं और (शायद इसलिए) बहुत अच्छा कहते हैं.
ग़ज़ल के मैदान में उसने वह सब कुछ कहा है, जिसके लिए बाज़ तरक़्क़ीपसंद शायर सिर्फ नज़्म का ही पैराया ज़रूरी और नागु़जीर (अनिवार्य) समझते हैं. सही तौर पर उसने ग़ज़ल के क़दीम शीशे में एक नई शराब भर दी है.' क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार की यह बात सही भी है. मजरूह की एक नहीं, कई ऐसी ग़ज़लें हैं जिसमें विषय से लेकर उनके कहन का अंदाज़ निराला है.
मसलन 'सर पर हवा-ए-ज़ुल्म चले सौ जतन के साथ/अपनी कुलाह कज है उसी बांकपन के साथ.', 'जला के मश्अले-जां हम जुनूं-सिफात चले/जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले.' मजरूह, मुशायरों के कामयाब शायर थे. ख़ुशगुलू (अच्छा गायक) होने की वजह से जब वे तरन्नुम में अपनी ग़ज़ल पढ़ते, तो श्रोता झूम उठते थे. ग़ज़ल में उनके बग़ावती तेवर अवाम को आंदोलित कर देते. वे मर मिटने को तैयार हो जाते.
मजरूह सुल्तानपुरी के कलाम में हालांकि ज्यादा ग़ज़लें नहीं हैं. उनकी किताब ‘ग़ज़ल’ में सिर्फ़ 50 ग़ज़लें ही संकलित हैं, लेकिन इन ग़ज़लों में से किसी भी ग़ज़ल को कमजोर नहीं कह सकते. उन्होंने अदबी कलाम कम लिखा, लेकिन बेहतर और लाजवाब लिखा. मिसाल के तौर पर उनकी एक नहीं, ऐसी कई ग़ज़लें हैं जिनमें उन्होंने समाजी और सियासी मौज़ूआत को कामयाबी के साथ उठाया है.

इनमें उनके बगावती तेवर देखते ही बनते हैं. मुल्क की आज़ादी की तहरीक में ये ग़ज़लें, नारों की तरह इस्तेमाल हुईं. 'सितम को सर-निगूं, जालिम को रुसवा हम भी देखेंगे/चले ऐ अज़्मे बग़ावत चल, तमाशा हम भी देखेंगे.' मजरूह सुल्तानपुरी की शुरुआती दौर की ग़ज़लों पर आज़ादी के आंदोलन का साफ़ असर दिखलाई देता है. दीगर तरक़्क़ीपसंद शायरों की तरह, उनकी भी ग़ज़लों में मुल्क के लिए मर-मिटने का जज़्बा नज़र आता है.
ये ग़ज़लें सीधे-सीधे अवाम को संबोधित करते हुए लिखी गई हैं. 'यह जरा दूर पे मंज़िल, यह उजाला, यह सुकूं/ख़्वाब को देख अभी ख़्वाब की ताबीर न देख/देख जिंदां से परे, रंगे-चमन, जोशे-बहार/रक्स करना है तो फिर पांव की ज़ंजीर न देख.' अवामी मुशायरों में तरक़्क़ीपसंद शायर जब इस तरह की ग़ज़लें और नज़्में पढ़ते थे, तो पूरा माहौल मुल्क की मुहब्बत से सराबोर हो जाता था. लोग कुछ कर गुज़रने के लिए तैयार हो जाते थे.
अप्रत्यक्ष तौर पर ये अवामी मुशायरे अवाम को बेदार करने का काम करते थे. ख़ास तौर से मजरूह की शायरी उन पर गहरा असर करती. लंबे संघर्षों के बाद, जब मुल्क आज़ाद हुआ तो मजरूह सुल्तानपुरी ने इस आज़ादी का इस्तक़बाल करते हुए लिखा, 'अहदे-इंक़लाब आया, दौरे-आफ़ताब आया/मुन्तज़िर थीं ये आंखें जिसकी एक ज़माने से/अब ज़मीन गायेगी, हल के साज़ पर नग़मे/वादियों मे नाचेंगे हर तरफ तराने से.'
मजरूह सुल्तानपुरी ने साल 1945 से लेकर साल 2000 तक हिंदी फ़िल्मों के लिए गीत लिखे. अपने पचपन साल के फ़िल्मी सफ़र में उन्होंने 300 फ़िल्मों के लिए तक़रीबन 4000 गीतों की रचना की. फ़िल्मी दुनिया में इतना लंबा समय और इतने सारे गीत किसी भी गीतकार ने नहीं रचे हैं.
फ़िल्मी गीतों ने मजरूह सुल्तानपुरी को ख़ूब इज़्ज़त, शोहरत और पैसा दिया. बावजूद इसके वे अदबी काम को ही बेहतर समझते थे. फ़िल्मी गानों की मसरूफ़ियत के चलते, वे ज़्यादा अदबी लेखन नहीं कर पाये. लेकिन उन्होंने जो कुछ भी लिखा, वह उन्हें ऊंचे ग़ज़लकार के दर्जे में शामिल करने के लिए काफ़ी है. फ़िल्मों में जब भी मजरूह को गुंजाइश मिली, उन्होंने गीत की बजाय ग़ज़ल को आगे बढ़ाया और ये ग़ज़लें ख़ूब मक़बूल भी हुईं.
फ़िल्मों में ऐसी ही उनकी कुछ मशहूर ग़ज़लें हैं, 'रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह/बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गु़नहगारों की तरह.' (फ़िल्म : ममता), 'हमीं करें कोई सूरत उन्हें बुलाने की/सुना है उनको तो आदत है भूल जाने की.' (फ़िल्म : एक नज़र) इनमें भी फ़िल्म ‘दस्तक’ की ये ग़ज़ल, 'हम हैं मता-ए-कूचा-ओ-बाज़ार की तरह/उठती है हर निगाह खरीदार की तरह.', तो जैसे पूरी फ़िल्म का केन्द्रीय भाव प्रकट कर देती है.
अदब की ख़िदमत और फ़िल्मी दुनिया में लिखे गीतों के लिए मजरूह सुल्तानपुरी, अपनी ज़िंदगी में ही कई अवार्डों से नवाज़े गए. ‘ग़ालिब अवार्ड’, ‘इक़बाल सम्मान’ और ‘वली अवार्ड’ जैसे अदबी अवार्डो के अलावा उन्हें फिल्म ’दोस्ती’ के गाने ’चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे’ के लिए फ़िल्मफ़ेयर अवार्ड मिला. मजरूह सुल्तानपुरी फ़िल्मी दुनिया में ऐसे गीतकार थे, जिन्हें सबसे पहले ‘दादा साहब फाल्के अवार्ड’ मिला.
24 मई, साल 2000 को 80 साल की उम्र में वे इस फ़ानी दुनिया से हमेशा के लिए रुख़्सत हो गए. मजरूह सुल्तानपुरी भले ही जिस्मानी तौर पर हमसे जुदा हो गए हों, पर उनकी शायरी-गीत आज भी हवाओं में ये सदा दे रहे हैं, 'हमारे बाद अब महफ़िल में अफसाने बयां होंगे/बहारें हम को ढ़ूॅंढ़ेंगी न जाने हम कहॉं होंगे.'