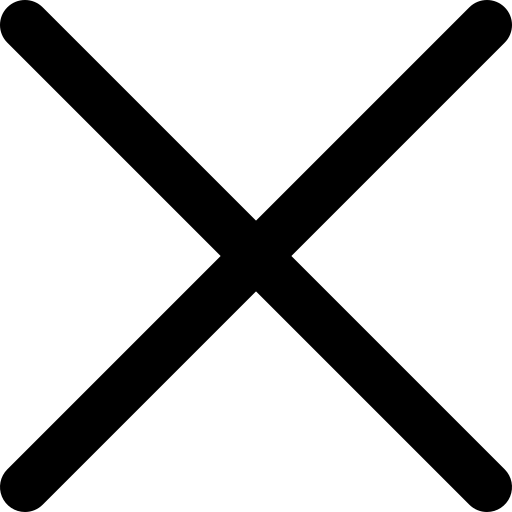अब्दुल्लाह मंसूर
क़ौम के बनाए ढाँचे में पसमांदा मुसलमान तब तक गुमनाम रहे जब तक लोकतंत्र में हर एक वोट को एक समान महत्व नहीं मिला.आज भी अशराफ़ उलेमाओं, बादशाहों की 10वीं-11वीं पीढ़ियाँ अपने इतिहास को पूरे मुसलमानों के इतिहास के रूप में पेश कर रही हैं.वो इतिहास जो पसमांदा के लिए अपमान का इतिहास रहा है.आज पसमांदा आंदोलन न केवल अशराफ मुसलमानों के आधिपत्य पर सवाल उठा रहा है, बल्कि इतिहास को फिर से लिखने और ‘कुलीन’ अल्पसंख्यक राजनीति के प्रतीकों और मुहावरों को बदलने का भी प्रयास कर रहा है.
हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि तथाकथित भारत के मुस्लिम काल में पसमांदा जातियाँ जैसे लालबेगी, हलालखोर, मोची, पासी, भंट, भटियारा, पमरिया, नट, बक्खो, डफली, नालबंद, धोबी, साई, रंगरेज, चिक, मिर्शीकर और दर्जी आदि की स्थिति क्या थी उनका इतिहास कहाँ है?
इतिहास की साम्प्रदायिक व्याख्या का लाभ
स्टीव बिको कहते हैं ‘दमनकारी के हाथ में उत्पीड़न का सबसे ताकतवर हथियार पीड़ित का दिमाग है.पसमांदा समाज सदियों से अशराफ़ों के अनुभव को अपना अनुभव, उन की जीत को अपनी जीत और उनके झूठे किस्से को अपना इतिहास मानता रहा है.
इस का नतीजा यह हुआ कि कई उलेमा, बादशाह और सुल्तान ऐतिहासिक पुरुष न हो कर दिव्य पुरुष बन गए.इस तरह बादशाहों को मुस्लिम आस्था का विषय बना दिया गया.आस्था का विषय बनाने का लाभ यह है कि सारे प्रश्न रोक दिए जाएंगे, अब कोई शोध उन की छवि को धूमिल नहीं कर सकता.अगर ऐसा किसी ने किया तो उसे लोग ईशनिंदा की तरह दिखने लगेंगे.
अधिकतर अशराफ़ इतिहासकारों, शायरों, लेखकों ने मध्यकाल के इतिहास को अपने सुनहरे काल की तरह पेश किया.ऐसा ही अशराफ इतिहासकारों और कवि लेखकों ने प्राचीन भारत के इतिहास के साथ किया.इन्होंने सुल्तानों और बादशाहों को पूरे मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि के रूप में दिखाया.यही वजह है कि दशकों से भारत में कट्टर हिंदुत्ववादी शक्तियों ने ‘मुस्लिम पहचान’ को निशाना बनाने के लिए भारत के ‘मुस्लिम इतिहास’ और ‘मुस्लिम बादशाहों’ को निशाना बना रहे हैं.
पर क्या वाक़ई यह सुल्तान और बादशाह भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? इस संदर्भ में पसमांदा अपनी मुस्लिम पहचान के कारण दक्षिणपंथी संगठनों के निशाने पर आ जाता है, उस के इतिहास को, उस के दुःख को, उस के शोषण को तथाकथित भारत के मुस्लिम इतिहास की चादर में छुपा लिया जाता है.जिसे अशराफ़ लेखक और कवि मुसलमानों का स्वर्णिम युग कहते हैं, वही युग पसमांदा मुसलमानों के लिए दासत्व, अवमानना व अवनति का प्रतीक था.
ऐतिहासिक दृष्टि से हम इस बात को सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि इन ‘मुस्लिम’ और इन के विदेशी अमीरों की राजनीतिक-धार्मिक-सांस्कृतिक स्वामिभक्ति भारत से बाहर थी.जिस तरह इतिहास में हिन्दू शासन या हिन्दू पहचान प्रमुख न हो कर जाति, नस्ल, देश, राज्य की पहचान प्रमुख हुआ करती थी.
उसी तरह मुस्लिम पहचान कभी भी कोई एक पहचान नहीं रही है.यहाँ भी अरब, तुर्की, ख़िलजी, लोदी आदि काल रहा है.इन मुसलमान बादशाहों की विदेशी नस्ल की पहचान हमेशा ही प्रमुख बनी रही है.स्थानीय संस्कृति को यह हमेशा ही घृणा की दृष्टि से देखते रहे.इन की भाषा विदेशी रही जिसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था.
दरबारी भाषा कभी भी पसमांदा मुसलमानों की भाषा नहीं र., इनकी स्थानीय भाषा को हमेशा ही हीन समझा गया.इन अशराफों के दरबार के रीति-रिवाज विदेशी रहे.अशराफ़ मुसलमानों में जातीय/नस्लीय गर्व इतना था और है कि वह अपने विदेशी मूल का शजरा (परिवार वृक्ष) रखते हैं.अपने नामों के साथ अपने पूर्वजों के नाम और यहाँ तक कि अपने विदेशी शहर का नाम भी लगाते थे.
(यहाँ यह भी ज्ञात रहे कि लोधी और सूरी शासकों ने भारतीय संस्कृति को महत्व दिया क्योंकि अरब-ईरान की जगह अफ़ग़ानिस्तान से होने के नाते इन को भी हीन समझा जाता था) अशराफ़ लेखकों, कवियों, इतिहासकारों और सवर्ण-अशराफ़ फ़िल्म डायरेक्टरों ने इन्हीं अशराफ़ संस्कृति को ‘मुसलमानों की संस्कृति’ के रूप में पेश किया.
पसमांदा मुसलमानों के साथ दिक्कत यह हुई कि वह इस विदेशी संस्कृति को अपनाने के चक्कर में वह अपनी स्थानीय संस्कृति से कट गए और इन विदेशी मुसलमानों ने इन्हें कभी आत्मसात भी नहीं किया.जब भी इन अशराफ़ मुसलमानों पर कोई मुसीबत आती तो इसकी वजह उलेमा भारतीय पसमांदा मुसलमानों की हिन्दू रीति-रिवाजों के कारण ईमान में आई कमी को दर्शाते हैं.

नस्लीय-जातीय सर्वोच्चता की मानसिकता
अशराफ़ बार-बार यह तर्क देते हैं कि मुसलमानों (अशराफ़) की हुकूमत 800साल तक भारत में रही.यह हमेशा खुद को भारत से बाहर का बता कर पेश करते हैं.साथ ही वह यह भी तर्क देते हैं कि अगर यह बादशाह चाहते तो सभी हिंदुओं को मुसलमान कर देते.
मतलब उन्होंने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया.अब सवाल यह उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया! क्या वह सभी धर्मनिर्पेक्ष थे या इस्लाम की तालीमात को मानते थे (तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ मेरा दीन मेरे साथ) या फिर इसके पीछे कोई आर्थिक कारण और निम्न जातियों के प्रति इन की तिरस्कार की भावना रही है.
‘मुस्लिम’ सुल्तानों और बादशाहों के प्रशासन को अगर हम देखें तो पाते हैं कि उन के प्रशासन में कोई भी पसमांदा मुसलमान नज़र नहीं आता.यहाँ तक कि भारत के ऊँची जातियों से धर्मांतरीत मुसलमान भी प्रारम्भ में उनके प्रशासन में आप को नज़र नहीं आएंगे.
इतिहासकार मुबारक अली अपनी किताब 'तारीख तहकीक के नए रुहजानात' में लिखते हैं कि जब इस्लाम ईरान में पहुंचा तो उसके सामाजिक सांचे में ढल गया.ईरानी समाजी मॉडल में पसमांदा लोगों को को हिकारत की नज़र से देखा जाता था.इन लोगों में कसाई, कबाड़ी, जुलाहे, मछुआरे, मवेशियों का व्यापार करने वाले शामिल थे.
उनके घटिया नस्ल का माना जाता था।.ईरानी समाज-संस्कृति में किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व देखने के लिए सबसे पहले उसका खानदान और खानदान की सर्वोच्चता को देखना होता था.भारत के सुल्तान और मुगल फारसी भाषा के साथ ईरानी संस्कृति को साथ लेकर आए जो पहले से ही भेदभाव पर आधारित थी.निज़ाम-उल-मुल्क तोसी ने सियासत नामा में लिखा है कि दिल्ली के सुल्तानों ने ईरानी राजाओं की विचारधारा और सभ्यता को स्वीकार कर लिया था.
राज्यकीय विभागों और उच्च पदों पर तो तुर्को का ही वर्चस्व था.भारतीय मूल(पसमांदा) के मुसलमान विभागों(शासकीय) और पदों से दूर ही रहें। केवल मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का वह पहला बादशाह था जिसने भारत के योग्य व्यक्तियों को जो मुसलमान हो चुके थे कुछ उच्च पद दिए,
हालांकि यह बात बाहर से आये हुए मुसलमानो की इच्छा के विरुद्ध होती थी, जो बिना किसी गैर (भारतीय मूल के लोग) के मिश्रण के शासन के व्यवस्था प्रणाली में अंदर तक पहुँच रखते थे, और उन्होंने जातिगत अस्मिता के गैर इस्लामी विचार की तरफ झुकाव को हवा दी.
सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश और गयासुद्दीन बलबन स्थानीय मुसलमानों को घृणा की नजर से देखते थे.अल्तमश ने 33मुसलमानों (भारतीय मूल के पसमांदा) को शासकीय पदों से केवल इसलिए बर्खास्त कर दिया कि उनका संबंध किसी उच्च वर्ग के परिवार से नहीं था.
बलबन ‘निचले’ स्तर के मुसलमानों (पसमांदा) को सरकारी पदों से बर्खास्त करते हुए कहा था कि मैं जब नीच परिवार के किसी सदस्य को देखता हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है.नस्ल और जाति के आधार पर यह अपने मनसब/पद बाँटा करते थे.अगर कोई स्थानीय मुसलमान ऊँचे पद पर पहुँचने की कोशिश भी करता तो उसे हटा दिया जाता था.
मसूद आलम फलाही अपनी किताब ‘ज़ात-पात और मुसलमान’ में लिखते हैं सुल्तान इल्तुतमिश और बलबन जो गुलाम वंश से थे, इन के वक़्त में किसी ‘निचली’ जाति के व्यक्ति (चाहे वह मुसलमान ही क्यों न हो ) की ऊँचे पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती थी.
अगर यह मालूम हो जाए कि कोई पदाधिकारी निचली जाति का है तो उसे पदच्युत कर दिया जाता था.बलबन ने तो बाकायदा एक विभाग ‘नकाबत’ बनाया था जो पदाधिकारियों की जाति की जाँच करता था। बलबन का मानना था कि शासन के दायित्व को अकुलीन व्यक्तियों में नहीं बाँटा जा सकता है.
सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के काल में निजामुल मुल्क(एक उच्च शासकीय पद) जुनैदी(कोरी/जुलाहा) ने जमाल मरज़ूक़ (जो पसमांदा जाति से थे) को एक पद देना चाहा तो मंत्री ख्वाजा अज़ीज़ बिन बेहरोज़ ने एक फारसी का शेर पढ़ा जिसका अर्थ है-‘नीच के हाथ में कलम ना दें अगर उसमे साहस आ गया तो काबा में लगे काले पत्थर को इस्तिन्जा का ढेला* बना देगा.’ *मुस्लिम मूत्र त्यागने के बाद पानी से धोते है या मिट्टी के ढेले से सुखाते हैं.इसी को इस्तिनजा कहते हैं.
यह भी ग़ौर करने वाली बात है कि शुरुआत के सुल्तान दास हुआ करते थे.इरफ़ान हबीब लिखते हैं कि दासों को जातिविहीन माना जाता था.इस्लाम क़ुबूल करने के बाद उन्हें किसी भी काम में लगाया जा सकता था.वह जिस काम से जुड़ते थे कालांतर में उन की जाति वही गिनी जाती थी.
यह सुल्तान ग़ुलाम होने के बावजूद ख़ुद को विदेशी शासक वर्ग का ही मानते थे और भारत की पसमांदा जातियों से नफ़रत करते थे.एक बात और समझें.साम्राज्य को भाइयों के बीच बाँट कर शासन करना एक खतरनाक काम था.इसलिए राजा/सुल्तान अपने भाइयों की जगह दासू को सत्ता सौंप देते.यह दास जीते गए क्षेत्र पर सुल्तान के नौकरशाह के रूप में काम करते थे.जब भी सुल्तान का मन होता है उनसे सत्ता ले सकता था जबकि भाइयों को सत्ता देने का अर्थ था साम्राज्य में बंटवारा.
विदेशी मुसलमानों की श्रेष्ठता की अवधारणा ने स्थानीय मुसलमानों की प्रगति के सारे रास्ते बंद कर दिए और उन्हें समाज की निचली सीढ़ी पर बने रहने को बाध्य किया। इतिहासकार मुबारक़ अली अपनी किताब ‘इतिहास का मतान्तर’ में लिखते हैं कि उन विदेशी मुसलमानों के बच्चों तक को घृणा की नजर से देखा जाता था जिन की माताएँ स्थानीय होती थीं.
उदाहरण के तौर पर दक्षिण भारत में अरब के आदिवासियों को ‘नवैत’ कहा जाता था.जब उनमें से कुछ ने तमिल स्त्रियों से विवाह कर लिया तो उन के द्वारा पैदा हुए बच्चों को ‘लब्बी’ कहा गया.उन्हें अरब परिवारों के बराबर नहीं माना गया.कोरोमंडल में बसने वाले अरब, स्थानीय मुसलमानों की सामाजिक-सांस्कृतिक परम्परा को ग़ैर-इस्लामी मानकर घृणा करते थे.
इतिहासकार मुबारक अली अपनी एक और किताब 'तारीख तहकीक के नए रुहजानात' में लिखते हैं कि मालाबार के अरब व्यापारियों में मुताह (contractual marriage) का चलन था.जिन औरतों से यह मुताह विवाह करते थे शायद उनका सम्बंध निम्न जाति से होता होगा.
इनसे होने वाले बच्चे माँ से जोड़ कर देखे जाते थे न की बाप से इसी वजह से इन्हें मोपला, मापला या महापला कहा जाता था.जिसका अर्थ बड़ा बच्चा और माँ का बच्चा होता है.मुबारक़ अली आगे लिखते हैं कि जब सिकंदर लोदी के उत्तराधिकार का सवाल उठा तो अफ़ग़ान संभ्रांत वर्ग ने इस आधार पर उस का विरोध किया कि उसकी माँ स्थानीय थी तथा सुनारों की जाति की थी.
सिंध में मुज़फ्फर खान तुर्क को गद्दी का उत्तराधिकारी इसलिए नहीं बनने दिया गया क्योंकि उस की माँ सिंधी ‘झरिया’ जनजाति की थी.मिर्ज़ा बाक़ी तरखन जिस की माँ एक सिंधी थी, को हिकारत से ‘सिंधी बच्चा’ कहा जाता था.

पसमांदा समाज का तिरस्कार
पसमांदा मुसलमानो के साथ ना सिर्फ सामाजिक आधार पर घृणा और नीचतापूर्ण व्यवहार किया गया, बल्कि सरकारी तौर पर भी उनसे नफरत की गई जैसा कि मुग़ल राजा अकबर ने कसाईयो और मछुआरों के लिए राजकीय आदेश जारी किया था कि उन के घरों को आम आबादी से अलग कर दिया जाए.जो लोग इस जाति से मेलजोल, आना-जाना रखें उनसे जुर्माना वसूला किया जाए.
मसूद आलम फलाही अपनी किताब ‘हिन्दुस्तान में जात-पात और मुसलमान’ में एस.सी. दुबे को नक़्ल करते हुए लिखते हैं कि अकबर ब्राह्मणों से धर्मांतरित हिन्दुओं को सैयद का दर्जा देता था.आगे वह अकबर का एक फ़रमान नक़्ल करते हैं जहाँ अकबर अपने आदेश में कहता है कि ‘शहरों में नीची क़ौम के लोगों को इल्म हासिल करने से रोक दिया जाए.
क्योंकि इन क़ौमों के इल्म हासिल करने से फ़साद पैदा होता है.’ ना सिर्फ पद और प्रोत्साहन में उच्च और निम्न का विभेद किया जाता था बल्कि सजा के निर्धारण में जातिगत श्रेणी के अनुसार भी भेद किया जाता था जैसा कि आईने अकबरी भाग-2, पेज संख्या 233पर उच्च और निम्न परिवार के सदस्यों पर अर्थदंड का विवरण कुछ इस तरह लिखा है.
अगर नीच श्रेणी का मलेछ किसी उच्च श्रेणी और उच्च परिवार के किसी व्यक्ति को अपशब्द कहे तो उससे अर्थदण्ड के रूप में साढ़े बारह दिरहम लिए जाएंगे, अगर बराबर श्रेणी के लोग एक-दूसरे को गाली दें तो उसका आधा और अगर उच्च श्रेणी वाला किसी को गाली दें तो उस से चौथाई वसूल किया जाएगा.
ऐसे और भी कई उद्धरण दिए जा सकते हैं यह बताने के लिए कि कैसे पसमांदा जातियों की दरिद्रता के लिए यह तथाकथित मुस्लिम बादशाह ज़िम्मेदार हैं.इरफ़ान हबीब अपनी किताब ‘भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा‘ में लिखते हैं; 11वीं सदी में अलबरूनी ने बुनकरों और मोचियों समेत आठ व्यवसायों को समाज-बहिष्कृत ‘अत्यंत’ (निकृष्ट) जातियों की श्रेणी में रखा था.
निकृष्ट स्थिति और गतिशीलता के अभाव के कारण दस्तकारों की प्रतिरोधक क्षमता ही कम हुई होगी और इस प्रकार उजरत रुपी लागत भी कम रही होगी.जाति प्रथा ग्राम समुदायों से राजस्व प्राप्त करने में तथा नगरों में उजरत-रुपी लागत को कम करने में सहायक थी.
इस लिए भारत के सभी मुस्लिम शासकों के पास उसे सुरक्षित रखने के पर्याप्त कारण थे.मुसलमानों में भी ‘कमीन’ समुदायों के रूप में निकृष्ट जातियों के प्रतिरूप विकसित हुए.ये समुदाय अछूत तो नहीं थे फिर भी इन को अपमान के भाव से देखा और दूर रखा जाता था.
‘मुस्लिम’ शासन व्यवस्था में सैयदों की स्थिति
उलेमाओं में एक बड़ा वर्ग सैयद उलेमाओं का था.सैयद मौलवियों ने झूठी कहानियां और हदीस गढ़ कर सैयदों की श्रेष्ठता को स्थापित किया.इस बात को मुस्लिम समाज में स्थापित कर दिया कि सैयद जन्म से ही श्रेष्ठ हैं.यही वजह है कि मुस्लिम शासक सादात (सैयद) परिवारों की ख़ास देखभाल करते थे.
काजी, मुफ्ती और सदर जैसे सारे ओहदे उन्हें दिए जाते थे.इस के अलावा ऊँचे प्रशासनिक पद भी उन्हें दिए जाते थे.उन्हें जागीरें, वज़ीफ़े एवं छात्रवृत्तियां दी जाती थीं.शासक उन का सम्मान करते तथा उन के अपराध आम तौर पर क्षमा कर दिए जाते.हत्या के मामले में भी सैयद को मौत की सजा नहीं दी जाती थी क्योंकि सैयद का ख़ून बहाना शासक अपशकुन मानते थे.
इस नज़रिये का नतीजा यह हुआ कि सैयद वर्ग अत्यधिक सुविधा सम्पन्न बन गया.सारी सुविधाओं को एक छोटे से दायरे में सीमित रखने के लिए सैयदों ने अन्य जातियों एवं समूहों से संबंध विच्छेद कर लिया तथा दावा किया कि उन का रक्त शुद्ध है.खून को शुद्ध रखने के लिए वह कुफ़ू के सिद्धांत को इस्लाम में लेकर आए.
वह अपने परिवारों में शादियां करते तथा अन्य जाति समूहों से उन के आवास दूर होते.यहाँ तक कि उन के कब्रिस्तान भी अलग होते ताकि लोग आकर चढ़ावा चढ़ा सकें.मकबरे आमदनी के बड़े स्रोत होते हैं.इन असाधारण सुविधाओं के कारण बड़ी संख्या में सैयदों ने मध्य एशिया, ईरान तथा अरबी दुनिया से आना शुरू किया.
सदातों (सैयद) के इतने परिवार हो गए कि हर शहर और गाँव में एक-दो (सैयद) परिवार थे जिन के लिए वह गर्वित थे.[इतिहासकार मुबारक़ अली ‘इतिहास का मतांतर‘ पृष्ठ 50, 51] याद रहे सैयदवाद को उन लोगों की सहायता और सहयोग की ज़रूरत होती है, जिन लोगों पर यह विचारधारा शासन करती है.
पसमांदा मुसलमानों की सहायता और सहियोग से ही यह विचारधारा फल फूल रही है.एक विचारधारा के स्तर पर सैयदवाद सबसे पहले कुरान और हदीस के ज़रिए सैयदवाद( सैयद जन्म से श्रेष्ठ हैं) की वैधता को स्थापित करती है.एक बार इस्लामी वैधता स्थापित हो जाए तो सैयदवाद के आदेशों का पालन करना 85% पसमांदा मुसलमानों का नैतिक कर्तव्य बन जाता है.
सैयदवाद को फैलाने का काम विभिन्न माध्यमों से होता है.इसके लिए अलग अलग क्षेत्र के विशिष्ट कौशल और ज्ञान वाले लोगों की आवश्यकता होती है.जो अदब, मीडिया,सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मदरसों, विश्वविद्यालयों में सैयदवादी विचारधारा को स्थापित कर सकें.यही वह मनोवैज्ञानिक और वैचारिक कारक हैं जो पसमांदा मुसलमानों से सैयदवादी विचारधारा को मानने और उसे फैलाने को प्रेरित करते हैं.
याद रहे सत्ता-शक्ति के यह सभी स्रोत पसमांदा समाज की स्वीकृति और आज्ञाकारीता पर निर्भर करते हैं.सैयद वाले अपने भौतिक संसाधन के लिए मदरसों-मज़ारों (भारत उपमहाद्वीप में 99%मज़ार सैयदों की है) संगठनों, संस्थाओं पर अपना नियंत्रण मजबूत करता है.उन सभी लोगों को जो सैयद वाद की विचारधारा के खिलाफ हैं.उनको हर उस संस्था, संगठन में घुसने से रोका जाता है जिसपर सैयदवाद का कब्ज़ा है.

उलेमा की स्थिति
इस दौर में एक दूसरा प्रभावशाली ग्रुप उलेमाओं का था.उलेमाओं ने अपनी जातिवादी और साम्प्रदायिक नीतियों को लागू करवाने के लिए लगातार सुल्तानों-बादशाहों और संभ्रांत अशराफ़ों वर्ग को प्रभावित करते रहे.इतिहासकार मुबारक़ अली अपनी किताब ‘अलमिया-ए-तारीख़’ में लिखते हैं, “हिंदुस्तान में मुसलमान हुक्मरान ख़ानदानों के दौर-ए-हुकूमत में उलेमा हुकूमती इदारों की मदद से इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि मुसलमान समाज में रासिख़-उल-अक़ीदा की जड़ें मजबूत रहें ताकि इस की मदद से वह अपने असर और रसूख़ को बाक़ी रख सकें.
हुकूमतों ने उलेमा का तआवुन हासिल करने की ग़रज़ से जहां उन को हुकूमत के आला ओहदों पर फ़ायज़ किया (जैसे क़ाज़ी, हकीम आदि) वहाँ उसके साथ उन्हें मदद-ए-मआश (आर्थिक मदद) के नाम पर जागीरें दे कर आर्थिक रूप से ख़ुशहाल रखा.
इसलिए उलेमा और हुकूमत के दरमियान मफ़ाहिमत और समझौते के जज़्बात कायम रहे और उन्होंने इसके एवज़ उन हुकूमतों को इस्लामी क़रार दे कर मुसलमान रैयत को वफ़ादार रहने की तलक़ीन की। उलेमा का काम मसलों को हल करना नहीं बल्कि मसाइल पैदा करना था .
जैसे-जैसे मुस्लिम समाज को उन मसाएल में उलझाया जाता रहा वैसे-वैसे समाज में उलेमा का असर और रसूख़ बढ़ता रहा और वह मुस्लिम समाज के रहनुमा बनते रहे.इसलिए उन्होंने उन मसाइल का हल ढूँढने की कोशिश नहीं की बल्कि वक़्त के साथ-साथ नए मसाइल दरियाफ़्त करते गए.”
हम आज के दौर में भी यही सब कुछ देखते हैं.पसमांदा जातियों को शिक्षा और सत्ता से दूर रखने में भी इन की अहम भूमिका रही है.औरंगज़ेब द्वारा फतवा-ए-आलमगीरी का संकलन हुआ.(जिसके आधार पर मुफ़्ती फतवा देते रहे) जिसमें कुफु के नाम पर इस्लामी जातिवाद को और अधिक मजबूती प्रदान करते हुए प्रमाणित किया गया.
औरंगज़ेब की धर्मनिरपेक्षता केवल अशराफ-सवर्ण टाइप की धर्मनिरपेक्षता थी जिसमें बहुजन-पसमांदा के लिए कुछ नहीं था.औरंगज़ेब के शासन काल में, अकबर के शासन काल से भी अधिक ब्राह्मण और राजपूत शासन प्रशासन में रहें हैं.
सूफ़ीवाद के बारे में एक आम धारणा है कि यह इस्लाम की रूढ़ीवादी व्याख्या के विरुद्ध एक उदारवादी व्याख्या है.जो इस्लाम की रूढ़िवादी परंपरा प्रेम को महत्व देती जिसमें व्यक्ति की जाति-वंश लिंग, भाषा आदि कुछ भी मायने नहीं रखता पर इसके विरुद्ध सूफीवाद की जो पसमांदा व्याख्या है, वह सूफीवाद को सैयद जाति की Hegemony के रूप में देखती है.
पसमांदा दृष्टिकोण यह मानता है कि सूफीवाद सैयद जाति के जन्म आधारित श्रेष्ठता को स्थापित करने प्रमुख वाहक और पोषक है.जिसके जरिए इस्लामी मसावत (बराबरी) की जगह मुस्लिम समाज में ऊँच-नीच और जात-पात का जन्म हुआ है.मसूद आलम फलाही की किताब ‘हिंदुस्तान में ज़ात-पात और मुसलमान’ में फलाही बताते हैं कि कैसे भारत में इस्लाम आने से पहले ही मुस्लिम समाज में ऊँच-नीच का कंसेप्ट आ चुका था.
वह लिखते हैं कि खिलाफत की लड़ाई में कैसे झूठी हदीस गढ़ कर सैयदों के महत्व को बढ़ाया गया ताकि सत्ता पर उनका दैवीय अधिकार घोषित किया जा सके.जब सैय्यद जाति (बनू फातिमा) के लोग भौतिक सत्ता (खिलाफत) नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो ऐसी सूरत में आध्यात्मिक सत्ता की परिकल्पना की नींव डाली गई जो सूफी परम्परा कहलायी.सूफी परम्परा के खलीफा का सिलसिला अली से जाकर मिलता है,
फिर अली( र० अ०) से मुहम्मद( स०अ०व०) में मिल जाता है.सूफीवाद में अली को इस्लाम का पहला खलीफा माना जाता है.इस तरह सूफ़ीवाद भी खिलाफत की सत्ता संघर्ष में शिया पक्ष के साथ अपना संबंध जोड़ता है.जो खिलाफत पर वंश और जन्म आधारित श्रेष्ठता यानी अली (रज़ी) की नस्ल से सैयद जाति की वकालत करता है.
इस तरह हम देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास नस्लवादी जातिवादी इतिहास है.इस तथ्य के बावजूद कि इस्लाम समानता और भाईचारे को रेखांकित करता है.राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास की अनुपस्थिति भी एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ है जिसमें पसमांदा समाज का शोषण साफ झलकता है.
यह सवाल तो पूछा ही जा सकता है कि मुस्लिम मुल्कों में गुलामी प्रथा का खात्मा 1500साल के इस्लाम के अस्तित्व के बाद भी पिछली सदी में ही क्यों मुमकिन हुआ? हर व्यवहारिक मसले के लिए हमारा पाला कुरान शरीफ से नहीं उसकी व्याख्या से पड़ता है.
आज जब हम लोकतंत्र में 85%मुस्लिम समाज के पसमांदा की नुमाइंदगी तलाश करते हैं तो अशराफ राजनीति और उनके शाही मुद्दों के शोर के पीछे उन मुद्दों की चीख सुनाई देती है जिस पर पसमांदा हालात ज़ाहिर होते हैं.ये हालात जो पसमांदा समाज अब बदलने को बेचैन है.
उम्मीद है कि पसमांदा अपने इतिहास से सबक लेकर अपने वर्तमान को बदल पाएगा और अपनी जड़ें भारत के अंदर तलाश करेगा ताकि एक ऐसा वर्तमान बना सके जो राष्ट्रवाद और भारतीय एकता, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत कर सके। अंत: में अपनी एक कविता से बात समाप्त करना चाहता हूँ:-
मैं पसमांदा हूँ
समय के चक्र से विद्रोह करता
हताशा और निराशा के बीच पनपता हुआ एक पौधा
मैं विद्रोह की वह कर्कश आवाज़ हूँ
जिसे नहीं सुना तुमने कभी
नहीं देखा हम को कभी अपने 'कौम' के बनाए हुए ढांचे में ?
तुम्हारे 'इस्लामिक इतिहास' में हम कहाँ हैं ?
क्या दर्ज किया है तुमने हमारा इतिहास ?
अपने बादशाहों-सुलतानों के इतिहास के साथ ?
क्या दिखाई देती है मेरी पहचान तुम्हारे 'उर्दू अदब' में ?
मेरी भूख मेरी लाचारी मेरी हताशा पर
क्या लिखें हैं तुमने कोई गीत गाई है कोई ग़ज़ल ?
पर आज जब हम सुनाते हैं अपना दर्द
तुम नकार देते हो इसे 'फितना' कह कर
यह धूर्तता सीखी हैं तुमने अपने पुरखों से
और हमने सीखा है असम्भव परिस्थितियों में जीवित रहना
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
संदर्भ :
1- मुबारक अली, इतिहास का मतांतर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला संस्करण २००२
2- मुबारक अली, ‘अलमिया-ए-तारीख़, तारीख़ पब्लिकेशन, लाहौर, पाकिस्तान, संस्करण १९९४
3- इरफ़ान हबीब, भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा,पीपुल्स पब्लिशिंग हॉउस, संस्करण २००६
4- मसऊद आलम फलाही, हिंदुस्तान में ज़ात-पात और मुसलमान, आइडियल फाउंडेशन, मुम्बई, संस्करण २००९
5- मुबारक अली, तारीख तहकीक के नए रुहजानात,फिक्शन हाउस, लाहौर, संस्करण २००४
6-मौलाना कासिमी,डॉ० अब्दुल हक़, ज़ात-पात इस्लाम की नज़र में,
लेखक, पसमांदा एक्विस्ट तथा पेशे से शिक्षक हैं.Youtube चैनल Pasmanda DEMOcracy के संचालक भी हैं.