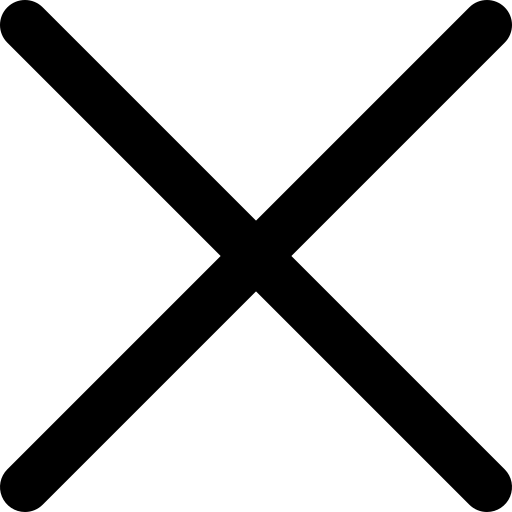आतिर खान
चालीस साल के अंतराल में दो ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुईं. पहली है कुली, जिसमें अमिताभ बच्चन ने इकबाल की भूमिका निभाई है. दूसरी है जवान, जिसमें शाहरुख खान ने विक्रम राठौड़ की भूमिका निभाई है. यह हमें क्या बताता है? भारतीय दर्शक फिल्म नायकों को उनके धर्म के बावजूद स्वीकार करते हैं, अभिनेताओं को भरोसेमंद और मनोरंजक होना चाहिए.
भारतीय दर्शक अच्छी तरह से पैक किए गए वीरतापूर्ण कृत्यों को पुरस्कृत करते हैं. यही कारण है कि शाहरुख खान थोड़े सुधार के साथ इन दिनों विक्रम राठौड़ के रूप में फिर से भरोसेमंद बन गए हैं.
उल्लेखनीय रूप से यह फिल्म कुछ ऐसी फिल्मों की पृष्ठभूमि में रिलीज हुई थी, जिन्होंने अच्छा व्यवसाय किया था, लेकिन उनकी प्रकृति धु्रवीकरण करने वाली थी, जैसे कि कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी. इससे यह आभास हुआ कि केवल ऐसी फिल्में ही चलन में आ सकती हैं. लेकिन भारतीय सिनेमा में हमेशा नवीनता की गुंजाइश रहती है.
अब फिल्म इतिहास के एक दिलचस्प किस्से पर थोड़ा पीछे चलते हैं. 1983 में अमिताभ बच्चन ने फिल्म कुली में इकबाल की भूमिका निभाई थी. फिल्म की शूटिंग के दौरान वह बुरी तरह घायल हो गए. उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि उनके बचने पर भी संदेह था.
तब भारतीय मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए मस्जिदों में प्रार्थना की थी. भारतीय फिल्म जगत की ऐसी कहानियां वाकई इसे दिलचस्प बनाती हैं.
बॉलीवुड के गीत और नृत्य के अलावा, जॉनी वॉकर, उत्पल दत्त और परेश रावल ने अपने हास्य प्रदर्शन से सभी भारतीय दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है. बॉलीवुड न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि एक मंच भी है, जो जनता के बीच जनमत बनाता है और लोगों के दिमाग में लंबे समय तक रहने वाली यादें छोड़ जाता है.
वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर बेमन से कहते हैं कि भारतीय फिल्म उद्योग बीते वर्षों के किरदारों को भूल गया है. सचमुच 1975 की फिल्म शोले में रहीम चाचा का किरदार निभाने वाले एके हंगल की यादें धुंधली होती जा रही हैं. युवा पीढ़ी को अतीत के ऐसे महान किरदारों के बारे में पता भी नहीं है.
रहीम चाचा के बेटे को गब्बर सिंह (अमजद खान द्वारा अभिनीत) नामक डाकू ने मार डाला था, जो बाहरी दुश्मन का प्रतीक था. जब शव गांव में आता है, तो शोकग्रस्त ग्रामीण क्रोधित हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनका दावा है कि विजय और वीरू, क्रमशः अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र द्वारा निभाई गई भूमिकाएं, दुष्ट गब्बर सिंह को खत्म करने के अपने मिशन में विफल रहे और इसलिए उन दोनों को गांव से निकाल देना जाना चाहिए.’’
रहीम चाचा ने हस्तक्षेप करते हुए ग्रामीणों से कहा कि यदि उनके सैकड़ों बेटे होंगे, तो वह उनका बलिदान कर देंगे, लेकिन विजय और वीरू को गांव छोड़ने की अनुमति नहीं देंगे, उन्हें बुरे आदमी गब्बर सिंह को निष्क्रिय करने के अपने मिशन को पूरा करने के लिए रुकना होगा.
हंगल के चरित्र ने बाहरी दुश्मन से सामूहिक रूप से लड़ने के लिए भारतीयों के अटूट विश्वास की भावना को दर्शाया, जिसका प्रतीक गब्बर सिंह है. यह किरदार प्रतीकात्मक वृहद स्तर पर अपने गांव और अपने देश की रक्षा करने की उनकी इच्छा का प्रतीक है. यह इस्लाम में बलिदान की सच्ची भावना को भी दर्शाता है. ऐसे किरदारों ने भावनाएं जगाईं और भारतीय समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत किया.
ये भी पढ़ें : उज्बेकिस्तान एक आदर्श मुस्लिम देश कैसे बना?
अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में मुस्लिम किरदार निभाए हैं, जिनमें सात हिंदुस्तानी में अनवर अली, ईमान-धरम में अहमद रजा और अंधा कानून में जां निसार खान शामिल हैं और इन सभी किरदारों को हिंदू और मुस्लिम दोनों दर्शकों ने समान रूप से पसंद किया.
इसी तरह, दिलीप कुमार और शाहरुख खान ने सबसे यादगार हिंदू किरदार निभाए हैं. ऋषि कपूर ने फिल्म ‘अमर अकबर एंथोनी’ में अकबर इलाहाबादी का किरदार निभाया था, यह मुस्लिम समाज को प्रतिबिंबित करने वाला एक और आकर्षक किरदार था. उनकी कव्वाली ‘परदा है परदा’ और उनकी कॉमेडी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुई. दुर्भाग्य से ऐसे पात्र अब विलुप्त हो गये हैं.
इन दिनों लोगों को जो याद है, वह केवल फिल्मों में मुस्लिम पात्रों का रूढ़िवादी चित्रण है. वैसे यह भारतीय सिनेमा में शोध करने वाले विद्वानों का पसंदीदा शोध विषय है. ऐसे सभी शोध बॉलीवुड की कड़ी आलोचना के साथ समाप्त होते हैं.
शिकायत यह है कि 9/11 हमले के बाद से मुसलमानों को या तो आतंकवादी या इस्लामवादी के रूप में दिखाया जाता है, और सकारात्मक किरदार नहीं. यह चलन हॉलीवुड फिल्मों से शुरू हुआ और इसने भारतीय सिनेमा उद्योग को भी प्रभावित किया. ऐसी फिल्में उस समय की वास्तविकताओं से प्रेरित हो सकती हैं, लेकिन प्रभाववादी बुरे चरित्रों की यादें लोगों के दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती हैं.
कथा को सही करने में फिल्म निर्माता करण जौहर का योगदान है. इस्लामवादियों और निर्दोष आम मुसलमानों के बीच अंतर को सामने लाने के लिए उन्होंने एक फिल्म बनाई, जिसका नाम था- ‘माई नेम इज खान.’ यह अपनी व्यावसायिक व्यवहार्यता और संदेश दोनों के मामले में काफी सफल रही.
इस फिल्म ने पश्चिमी दुनिया में प्रचलित इस्लामोफोबिया का मुकाबला किया. इसने समुदाय की धारणा को बेहतर बनाने की दिशा में सचेत रूप से एक सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया. दर्शकों ने इसे हाथों-हाथ लिया.
ये भी पढ़ें : लड़कियों को आगे बढ़ने से नहीं रोकता हिजाब, यूपी में बोली मुस्लिम जज
दिलचस्प बात यह है कि अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी में गणेश मंदिर का एक मार्मिक दृश्य है, जहां पुलिस बम की धमकी के कारण मंदिर में भक्तों को हटाती हुई दिखाई देती है.
एक आश्चर्यजनक प्रवेश में हम देखते हैं कि मुसलमानों का एक समूह भगवान गणेश की मूर्ति को सुरक्षित रखने और भक्तों को इमारत खाली करने में मदद करने के लिए मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहा है. मेल खाते संगीत से दृश्य में भावनाएँ तीव्र हो जाती हैं. यह दृश्य वास्तविक भारत को दर्शाता है, जहां संस्कृति इतनी आपस में जुड़ी हुई है कि देखभाल करने वाले भारतीयों को अलग करना असंभव है.
कुछ फिल्म समीक्षकों का कहना है कि 70 और 80 के दशक में मुस्लिम अंडरवर्ल्ड डॉन पर बॉलीवुड फिल्में बनाई जाती थीं. ऐसे पात्र मुंबई के कुछ सबसे कुख्यात गैंगस्टरों की सच्ची कहानियों से प्रेरित थे. फिर, उन फिल्मों ने एक स्थायी नकारात्मक प्रभाव छोड़ा.
हाल के दिनों में दो फिल्में कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी काफी विवादित रहीं. एक बड़े दर्शक वर्ग ने फिल्मों को पसंद किया, लेकिन एक बड़ी आबादी नाराज भी हुई. हालांकि फिल्म निर्माताओं ने फिल्में बनाने को लेकर अपनी सफाई दी है.
ये भी पढ़ें : मुसलमानों के लिए भारतीय उलेमा बना सकते हैं नया नैरेटिव
ये विवाद कोई नई बात नहीं है. अगर हम भारतीय टीवी और सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें, तो हमें ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे. गोविंद निहलानी की तमस 1947 के दंगा प्रभावित विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, यह फिल्म भारत में प्रवासी सिख और हिंदू परिवारों की दुर्दशा को दर्शाती है.
जब फिल्म 1988 में रिलीज हुई, तो समाज के एक बड़े वर्ग ने इसके सांप्रदायिक रंग के कारण फिल्म के कुछ हिस्सों को सेंसर करने की मांग की. इसकी रिलीज पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. लेकिन अदालत ने यह कहते हुए रोक हटा दी कि फिल्म में हिंदू और मुस्लिम दोनों के ‘कट्टरपंथियों’ के साथ समान व्यवहार किया गया है. फिल्म रिलीज हुई और इसे बड़ी सफलता मिली, इसे दूरदर्शन पर भी दिखाया गया. बाद में इसने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते.
अपने शोध ‘उदारीकरण के बाद के सिनेमा में भारतीय मुसलमानों की कल्पना’ में एक प्रसिद्ध विद्वान मैदुल इस्लाम, बॉलीवुड में कुछ मुस्लिम पात्रों के चित्रण की सराहना करते हैं. जैसे कि फिल्म - ‘सलीम लंगड़े पे मत रो’ में सलीम का किरदार. फिल्म के अंत में नायक सलीम को यह एहसास कराया जाता है कि ठग बनना सबसे आसान काम है, जबकि सबसे कठिन काम है सम्मान के साथ जीवन जीना.
इसी तरह, बलराज साहनी की ‘गरम हवा’ विभाजन के दर्द को दर्शाती है. फिल्म प्रतीकात्मक रूप से राजनीतिक संदेश देती है कि भारतीय मुसलमानों को अपनी वैध मांगों को उठाने और अपनी सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक शिकायतों को दूर करने के लिए एक प्रगतिशील राजनीतिक परियोजना के पीछे एकजुट होने की जरूरत है.
मैदुल नागेश कुकुनूर की फिल्म इकबाल में मुस्लिम नायक के चित्रण की भी सराहना करते हैं, जहां चरित्र में मुसलमानों से जुड़ी रूढ़िवादिता का कोई बोझ नहीं है.
ये भी पढ़ें : ‘जी20 इंटरफेथ शिखर सम्मेलन’ से भारत में धार्मिक सद्भाव और एकता वृद्धि संभव
‘चक दे इंडिया’ में शाहरुख खान का कबीर खान का चित्रण है. 3 इडियट्स के फरहान कुरेशी और फिल्म ‘जिंदगी मिलेगी ना दोबारा’ में फरहान अख्तर का इमरान कुरेशी का चित्रण, जहां वह अपने धर्म या सांस्कृतिक पहचान से कुछ भी नहीं जोड़ते हैं. ऐसे पात्र युवा भारतीय मुसलमानों की कल्पना को आकर्षित करते हैं, जो ऐसे पात्रों से संबंधित हैं, न कि पिछले वर्षों के इस्लामी कट्टरपंथियों या अंडरवर्ल्ड डॉन से.
एक फिल्म को बनाने के लिए पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम करती है. किसी भी रचनात्मक उद्योग की तरह, भारतीय फिल्म उद्योग भी बहुत समावेशी है और उन सभी को समान अवसर देता है, जिनके पास प्रतिभा है.
फिल्म निर्माण की प्रक्रिया उसकी संकल्पना के समय से ही शुरू हो जाती है, आजकल विषयों का चयन करते समय, विशेषकर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील फिल्मों पर विचार करते समय, उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है.
ये भी पढ़ें : भारतीय उलेमा को अपने विचारों में बदलाव की क्यों है जरूरत ?
फिल्म निर्माता अक्सर कहते हैं कि सिनेमा केवल वास्तविक दुनिया को दर्शाता है. ये बात काफी हद तक सच है. लेकिन कभी-कभी वास्तविक दुनिया को प्रतिबिंबित करते समय फिल्म निर्माताओं की ओर से सिनेमाई स्वतंत्रता लेते समय अति करने या अतिरंजित करने की इच्छा होती है. फिल्म निर्माताओं को नैतिकता पर सनसनीखेज हावी नहीं होने देना चाहिए.
अब जब वास्तविक दुनिया बदल गई है, तो फिल्म निर्माताओं को उन पात्रों की भी पुनर्कल्पना करनी चाहिए, जो समय के अनुरूप हों, अधिक प्रासंगिक और मनोरंजक हों.
कला रूप न केवल किसी विशेष समयावधि का वर्णन करते हैं, बल्कि सुधारात्मक प्रभाव भी डालते हैं. समय की मांग है कि एक एकीकृत कथा का निर्माण किया जाए, न कि विघटित करने वाली कथा का निर्माण किया जाए.