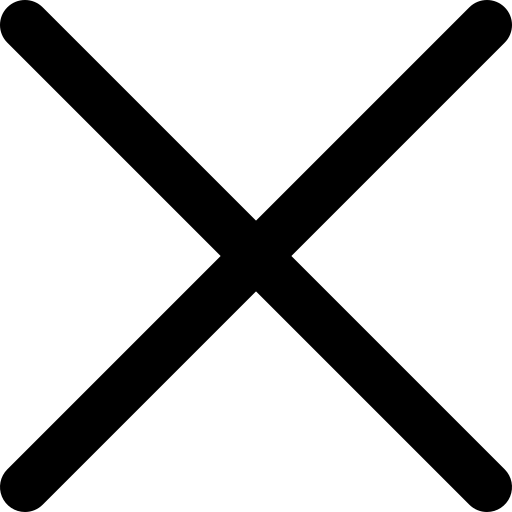डॉ. आमिर हुसैन
पारंपरिक शिल्प लंबे समय से पूर्वोत्तर भारत की आत्मा रहे हैं, जो पीढ़ियों से सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक जीवन दोनों को आकार देते रहे हैं. इतिहास, परंपरा और स्वदेशी ज्ञान के धागों से बुनी गई यह समृद्ध विरासत महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनी हुई है.
18-19 मार्च को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR), शिलांग द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका विषय था "पूर्वोत्तर भारत में शिल्प समुदाय और महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण", विद्वानों, कारीगरों, नीति निर्माताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को महिलाओं को सशक्त बनाने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में पारंपरिक शिल्प की भूमिका पर विचार करने के लिए एक साथ लाया.
शिल्प का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व
पूर्वोत्तर में शिल्प कौशल केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, यह सामुदायिक मूल्यों, पहचान और अंतर-पीढ़ीगत ज्ञान का प्रतीक है. शिल्प परंपराओं की सामूहिक प्रकृति समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देती है.
विशेष रूप से जातीय विविधता वाले क्षेत्र में. हथकरघा बुनाई और बांस के काम से लेकर टोकरी और झाड़ू बनाने तक के पारंपरिक शिल्प स्थानीय इतिहास और प्रथाओं के जीवंत संग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं.
प्रत्येक जातीय समूह इस जीवंत मोज़ेक में असाधारण रूप से योगदान देता है और शिल्प पहचान और गौरव का प्रतीक बन जाते हैं. जैसा कि मीतेई (2014) और केशब (2017) जैसे विद्वानों ने देखा है, शिल्प प्रथाएँ सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और सामाजिक सामंजस्य दोनों के रूप में काम करती हैं, विशेष रूप से आधुनिक परिवर्तनों के सामने स्वदेशी पहचान को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण हैं.
शिल्प उत्पादन के केंद्र में महिलाएँ
पूर्वोत्तर की शिल्प अर्थव्यवस्था में महिलाएँ केंद्रीय भूमिका निभाती हैं. आदिवासी और ग्रामीण परिवेश में, वे शिल्प ज्ञान की प्राथमिक रक्षक हैं, माँ से बेटी को कौशल हस्तांतरित करती हैं और सामुदायिक रीति-रिवाजों को बनाए रखती हैं.
पारंपरिक कपड़े बुनने से लेकर बांस की वस्तुएँ बनाने तक, महिलाएँ न केवल कलात्मक परंपराओं को बनाए रखती हैं, बल्कि आर्थिक जीविका की ज़िम्मेदारी भी उठाती हैं.
जैसा कि हज़ारिका (2006) ने देखा है. शिल्प गतिविधियाँ महिलाओं को आय-सृजन के अवसर प्रदान करती हैं जो वित्तीय स्वतंत्रता, बेहतर घरेलू कल्याण और सामाजिक मुक्ति में तब्दील हो जाती हैं.
पूरे क्षेत्र में, खास तौर पर ग्रामीण हाटों और साप्ताहिक बाज़ारों में, हस्तनिर्मित उत्पादों की बिक्री में महिलाएँ हावी हैं. उनकी कमाई सीधे बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा आवश्यकताओं और दैनिक घरेलू खर्चों का समर्थन करती है.
यह आत्मनिर्भरता घर के भीतर और समुदाय में उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाती है. यहाँ सशक्तिकरण केवल वित्तीय लाभ तक सीमित नहीं है. इसमें मनोवैज्ञानिक और संरचनात्मक सशक्तिकरण शामिल है जो नेतृत्व, आवाज़ और गरिमा की ओर ले जाता है..
शिल्प और कृषि के बीच अंतर्संबंध
पूर्वोत्तर में शिल्प कृषि चक्र से बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं. पहाड़ियों और मैदानों में, लोग मौसम के दौरान खेती करते हैं और ऑफ-सीजन में शिल्प-निर्माण की ओर रुख करते हैं.
यह चक्रीय आजीविका पैटर्न आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए जीवन की एक संतुलित लय प्रदान करता है. पर्यावरण बांस, जूट, लकड़ी और पौधे के रेशे (जैसे मेटेका) जैसे कच्चे माल प्रदान करता है, जो सभी टिकाऊ तरीके से उपयोग किए जाने पर नवीकरणीय हैं.
पर्यावरणीय क्षरण और वनों की कटाई अब इन संसाधनों को खतरे में डाल रही है. आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर रही है. कारीगरों पर तनाव डाल रही है.
पारंपरिक शिल्प के सामने चुनौतियाँ
हालाँकि शिल्प क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं, लेकिन आधुनिक युग में इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. अन्य भारतीय राज्यों से मशीन-निर्मित वस्तुओं के बढ़ने और चीन जैसे देशों से आयात ने स्थानीय बाज़ारों को बाधित कर दिया है.
रेशम बुनाई के लिए मशहूर असम के सुआलकुची जैसे स्थानों में सस्ते, बड़े पैमाने पर उत्पादित कपड़े की आमद ने बाज़ार में विभाजन पैदा कर दिया है. उच्च गुणवत्ता वाले हस्तनिर्मित उत्पाद निम्न-गुणवत्ता वाले डुप्लिकेट के साथ सह-अस्तित्व में हैं, जिससे मूल्य प्रतिस्पर्धा और मूल शिल्प का अवमूल्यन होता है.
नीति, शिक्षा और संस्थागत समर्थन की भूमिका
पारंपरिक शिल्पों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से, सहायक नीतियों और संस्थानों को विभिन्न स्तरों पर हस्तक्षेप करना चाहिए..
महिला कारीगरों को सफल उद्यमियों में बदलने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, ऋण तक पहुँच और बेहतर बाज़ार संपर्क आवश्यक हैं. क्लस्टर विकास, स्थानीय शिल्पों के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म और राज्य समर्थित प्रदर्शनियाँ और त्यौहार जैसी पहल बाज़ार तक पहुँच बढ़ाने में मदद कर सकती हैं.
डिज़ाइन नवाचार और मूल्य संवर्धन में प्रशिक्षण उत्पाद की अपील को बढ़ा सकता है और लाभप्रदता बढ़ा सकता है.शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. युवा पीढ़ी, हालाँकि तेज़ी से शिक्षित और आधुनिक जीवन शैली से परिचित हो रही है, उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत के मूल्य के प्रति संवेदनशील होना चाहिए.
स्कूलों और व्यावसायिक संस्थानों में शिल्प शिक्षा शुरू करने से यह उद्देश्य पूरा हो सकता है. संस्थान और विश्वविद्यालय, विशेष रूप से सामाजिक कार्य और विकास क्षेत्रों में, शिल्प आजीविका का समर्थन करने के लिए अनुसंधान, दस्तावेज़ीकरण और सामुदायिक जुड़ाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
शिल्प के माध्यम से महिला सशक्तिकरण
सशक्तिकरण बहुआयामी है.इसमें आय सृजन, सेवाओं तक पहुँच, निर्णय लेने में भागीदारी और सांस्कृतिक पुष्टि शामिल है. शिल्प गतिविधियाँ इन सभी आयामों को पूरा करती हैं..
जैसा कि जैन और ठक्कर (2019) का मानना है. शिल्प-आधारित आजीविका महिलाओं को पारंपरिक लिंग बाधाओं को तोड़ने, उनकी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने और आर्थिक और नागरिक जीवन में सक्रिय भागीदार बनने में मदद करती है.
कई आदिवासी क्षेत्रों में, महिलाएँ राजनीतिक रूप से भी अधिक सक्रिय हो रही हैं. अपने आर्थिक सशक्तिकरण का उपयोग व्यापक सामाजिक जुड़ाव की दिशा में एक कदम के रूप में कर रही हैं.
स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), सहकारी समितियों और ग्राम परिषदों में भागीदारी महिलाओं को सामूहिक कार्रवाई करने और अपने अधिकारों की वकालत करने की अनुमति देती है. सार्वजनिक स्थानों पर उनकी आवाज़ को तेज़ी से पहचाना जा रहा है.
समावेशी विकास के साधन के रूप में शिल्प
राजनीतिक रूप से शिल्प समुदायों के मूल्य को पहचानना भी उतना ही आवश्यक है. स्वदेशी संस्कृति में गहराई से निहित शिल्प कौशल सांस्कृतिक मुखरता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का माध्यम बन सकता है.
जब सरकार नीति और बुनियादी ढाँचे के माध्यम से कारीगरों का समर्थन करती है, तो यह न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है बल्कि सांस्कृतिक लोकतंत्र को भी पोषित करती है.
आगे की राह
सेमिनार ने शिल्प क्षेत्र को न केवल अतीत के अवशेष के रूप में बल्कि आधुनिक आजीविका, विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक जीवंत और विकसित योगदानकर्ता के रूप में फिर से कल्पना करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया..
हस्तनिर्मित और टिकाऊ वस्तुओं की बढ़ती मांग के साथ, पारंपरिक शिल्प एक आशाजनक भविष्य रखते हैं. हालांकि, नीति, सामुदायिक जुड़ाव और शैक्षिक एकीकरण के माध्यम से समय पर हस्तक्षेप के बिना यह समृद्ध विरासत खो सकती है.
इस क्षेत्र में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका परंपरा को सशक्तीकरण के साथ मिश्रित करने का एक शक्तिशाली अवसर प्रदान करती है. इसलिए शिल्प क्षेत्र की रक्षा, प्रचार और निवेश न केवल हमारी विरासत को संरक्षित करने के लिए बल्कि एक अधिक समावेशी, न्यायसंगत और आत्मनिर्भर पूर्वोत्तर भारत के निर्माण के लिए करें.
( डॉ. आमिर हुसैन,सहायक प्रोफेसर,सामाजिक कार्य विभाग,विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेघालय)