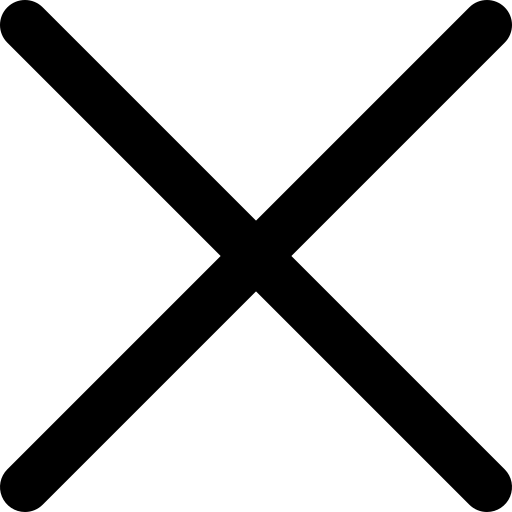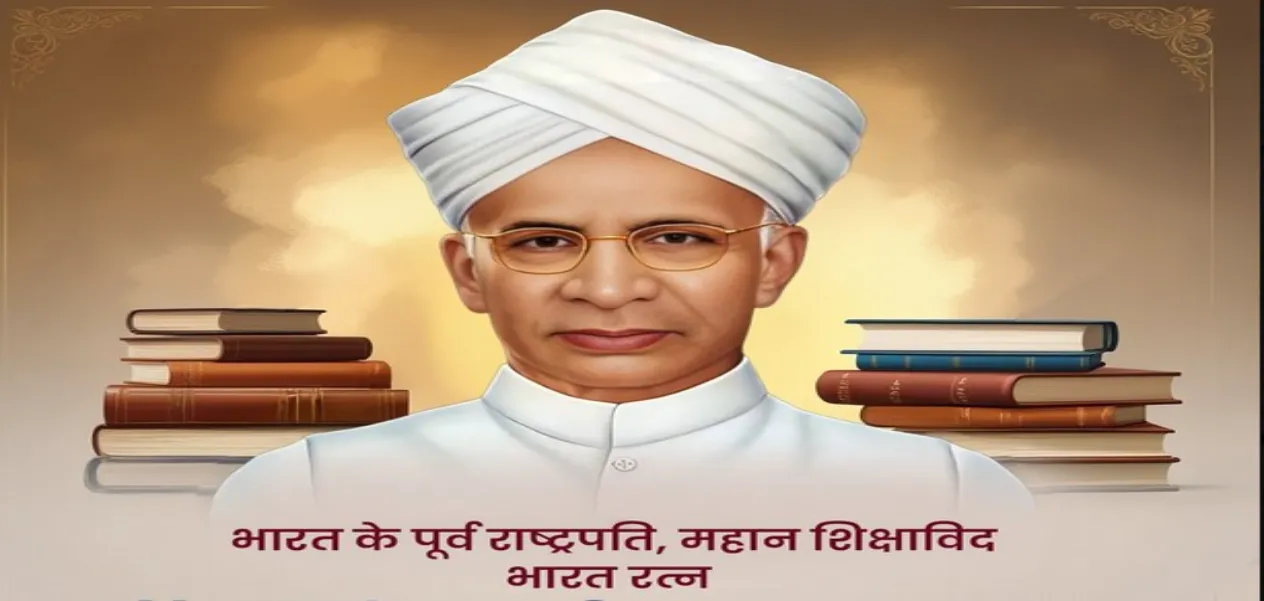
गुलाम कादिर
भारतीय दर्शन और धर्म के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाले डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन न केवल एक महान विद्वान, दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, बल्कि धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के एक गंभीर और संवेदनशील साधक भी थे. उनके लिए धर्मों की तुलना महज़ अकादमिक अभ्यास नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और अस्तित्वगत अन्वेषण का एक माध्यम थी.
राधाकृष्णन के लिए यह अध्ययन एक आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा था. अपनी आत्मकथात्मक रचना "सत्य की मेरी खोज" में उन्होंने बताया कि ईसाई धर्म द्वारा हिंदू धर्म की आलोचना ने उन्हें अपने स्वयं के धर्म की गहराइयों में उतरने के लिए प्रेरित किया.
छात्र जीवन में उन्होंने अपने धर्म की "जीवंतता" और "मृतता" को अलग-अलग पहचानने का प्रयास किया.उनके लेखन में बार-बार यह परिलक्षित होता है कि वे भारतीय (हिंदू, ब्राह्मणिक, बौद्ध) और पश्चिमी (यूनानी, ईसाई) धार्मिक परंपराओं की तुलना करते हैं.

उनका तुलनात्मक दृष्टिकोण केवल ऐतिहासिक और दार्शनिक न होकर आध्यात्मिक सहअस्तित्व की तलाश का भी प्रतीक था.डॉ. राधाकृष्णन ने अपनी कृतियों में स्पष्ट किया है कि तुलनात्मक धर्म का उद्देश्य केवल सहिष्णुता नहीं, बल्कि वास्तविक सम्मान और सहअस्तित्व की भावना विकसित करना है.
वे लिखते हैं कि यह दृष्टिकोण “ईश्वर की सार्वभौमिकता और मानव जाति के प्रति सम्मान” को गहरा करता है.उनका मानना था कि विभिन्न धर्म, यदि टकराव की स्थिति में नहीं रहना चाहते, तो उन्हें पूर्वाग्रहों और भ्रांतियों को तोड़ते हुए परस्पर समझ विकसित करनी होगी.
वे सभी धर्मों को एक ही सत्य की विविध अभिव्यक्तियाँ मानते थे. यह दृष्टिकोण उन्हें विस्तृत दृष्टिकोण और अंतर-धार्मिक संवाद की ओर ले जाता है.राधाकृष्णन के दर्शन में रहस्यवाद और मानवता की सार्वभौमिकता का गहरा प्रभाव है.
वे कहते हैं कि किसी भी धर्म को सही ढंग से समझने के लिए सहानुभूति आवश्यक है, केवल तर्क और आलोचना पर्याप्त नहीं.उन्होंने धर्मों के विकास को उनके सांस्कृतिक, सामाजिक, और बौद्धिक संदर्भों में देखा. उनके अनुसार, कोई भी धर्म पूर्ण नहीं है, बल्कि हर एक अपनी सीमाओं में सत्य की तलाश का प्रयास है.
इस विचार में वे जर्मन धर्मदर्शी ई. ट्रॉल्स्च के दृष्टिकोण से सहमत थे.उनकी तुलना मुख्यतः ब्राह्मणवाद और ईसाई धर्म के बीच केंद्रित रही है. बौद्ध धर्म उनके अध्ययन में उल्लेखनीय स्थान रखता है, जबकि इस्लाम पर उनके विचार अपेक्षाकृत सीमित हैं.
यह आश्चर्यजनक अवश्य लगता है, क्योंकि इस्लाम भारत के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है.इस चयनात्मकता का कारण उनके व्यक्तिगत अनुभव (हिंदू जन्म, ईसाई शिक्षा), बौद्धिक अभिरुचि तथा गूढ़ आध्यात्मिक दृष्टिकोण में देखा जा सकता है.
वे मानते थे कि हमें बाह्य धार्मिक संस्थाओं से आगे जाकर उस 'नामहीन' को पूजना चाहिए जो हर नाम से ऊपर है.राधाकृष्णन की दृष्टि में ब्राह्मणवाद मानव की आध्यात्मिक खोज का सबसे उच्च रूप हो सकता है. उनका यह विश्वास न केवल उनके दर्शन का हिस्सा है, बल्कि उनके जीवनानुभव और दार्शनिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति भी है.
हालाँकि, धर्मों के इतिहास का कोई गंभीर छात्र यह पूछ सकता है कि क्या उन्होंने ब्राह्मणवाद और ईसाई धर्म दोनों के साथ निष्पक्ष न्याय किया? यह प्रश्न गहन अध्ययन की माँग करता है. परंतु इसमें संदेह नहीं कि राधाकृष्णन का काम भारत की आत्मा, साहित्य और धर्म की राजनीतिक-सांस्कृतिक व्याख्याओं से गहराई से जुड़ा है.
डॉ. राधाकृष्णन का तुलनात्मक धर्म-दर्शन न केवल एक बौद्धिक प्रयास है, बल्कि सांस्कृतिक सहअस्तित्व, आध्यात्मिक एकता और वैश्विक भाईचारे की पुकार है. उनके विचार आज भी धार्मिक असहिष्णुता और सांप्रदायिकता के दौर में प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं.
वे हमें सिखाते हैं कि विविधता में एकता की खोज, संवाद में समाधान की संभावना, और हर धर्म में सत्य की झलक देखने की भावना ही एक सच्चे वैश्विक नागरिक और आध्यात्मिक साधक की पहचान है.
( लेखक वरिष्ठ टिप्पणीकार हैं. यह इनके विचार हैं.)