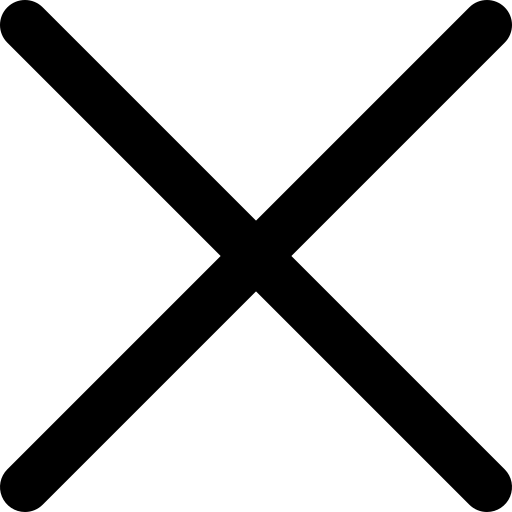शहाबुद्दीन अहमद
हमारे देश में महिलाएं शादी के बाद घर में अहम भूमिका निभाती हैं. शादी के बाद वह अपने पति की देखभाल, ससुराल की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चे पैदा करना, बच्चों का पालन-पोषण करना, घर चलाना आदि का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाती है. भारतीय संस्कृति में महिलाओं को उनके योगदान के लिए उच्च स्थान दिया गया है,लेकिन समय के साथ कई लोगों ने उन्हें वस्तु के रूप में उपयोग किया है.
कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं,जिन्होंने नारीवाद के नाम पर हाथ मिलाया है. हर धर्म में महिलाओं को ऊंचा दर्जा दिया गया है. प्रत्येक धर्म समाज में महिलाओं की आवश्यक भूमिका और बलिदान पर जोर देता है. हाल ही में हमारे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के अधिकारों पर एक अहम फैसला सुनाया है.
मोहम्मद अब्दुल समद नाम के एक शख्स ने फैमिली कोर्ट द्वारा जारी एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. समद ने तर्क दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को 1986 के अधिनियम की शरण लेनी चाहिए.
उन्होंने दावा किया कि यह अधिनियम सीआरपीसी की धारा 125 से अधिक स्वीकार्य है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर ऐतिहासिक फैसला सुनाया. फैमिली कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी तलाकशुदा पत्नी को 20,000 रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया था.

जवाब में, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरथाना और जस्टिस जॉर्ज मसीह की पीठ का फैसला न केवल मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, बल्कि अन्य धर्मों की महिलाओं के लिए भी एक मील का पत्थर था. इस फैसले में पीठ ने कहा, तलाकशुदा महिलाएं आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगने की हकदार हैं.
न्यायमूर्ति नागरथाना ने कहा, "हम इस प्रमुख निर्णय के साथ आपराधिक याचिका को खारिज करते हैं कि धारा 125 केवल विवाहित महिलाओं पर नहीं, बल्कि सभी महिलाओं पर लागू होगी." इस संबंध में, फैसले को धार्मिक मामलों पर भरण-पोषण के अधिकारों की सीमाओं को पार करके सभी विवाहित महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और वित्तीय सुरक्षा के सिद्धांतों को मजबूत करने के रूप में देखा जाता है.
शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीशों ने गृहिणियों द्वारा की गई आवश्यक भूमिका और बलिदान पर जोर दिया और भारतीय पुरुषों से अपनी पत्नियों पर भावनात्मक और वित्तीय निर्भरता को पहचानने का आग्रह किया.
उन्होंने कहा, “कुछ पतियों को यह पता नहीं है कि एक गृहिणी भावनात्मक होती है और अन्यथा उन पर निर्भर होती है. यह भारतीय पुरुषों के लिए परिवार के लिए गृहिणियों द्वारा की गई आवश्यक भूमिका और बलिदान को पहचानने का समय है”.

फैसला एक कड़ा संदेश देता है और यह स्पष्ट करता है कि भरण-पोषण दान का मामला नहीं है बल्कि सभी विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है. यह तलाकशुदा महिलाओं के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, उन्हें वह गरिमा और सम्मान देता है जिसकी वे हकदार हैं.
यह निजी कानूनों को लिंग-तटस्थ सीआरपीसी के तहत एक महिला के राहत के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने से भी रोकता है.
इस ऐतिहासिक फैसले के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी के तहत एक महिला के भरण-पोषण के अधिकार को शामिल कर लिया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि यह फैसला निजी कानून को खत्म या नकार देता है. इसलिए, इस निर्णय की एकता बनाए रखने के लिए धार्मिक नेताओं और धार्मिक समुदाय के नेताओं को निजी कानून के आधार पर इसके महत्व को कम करने से बचना चाहिए.
इस संबंध में, मुस्लिम महिलाओं को भी न्याय और समानता की दिशा में एक कदम के रूप में जश्न मनाना चाहिए, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो और उनकी आवाज़ स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो. सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण है.
वे अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कानूनी सहायता से स्वयं को सशक्त बना सकते हैं. यह एक प्रगतिशील पहल है जो लैंगिक समानता और न्याय को बढ़ावा देती है, जो धर्म की परवाह किए बिना सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि कर सकती है.
महिलाओं के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ऐतिहासिक फैसले दिए हैं. खासकर तलाकशुदा महिलाओं के मामले में. इस संबंध में ऐतिहासिक शाहबानू मामले का उल्लेख किया जा सकता है. 1985 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक ऐतिहासिक दिशानिर्देश था.

1985 के अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, लेकिन इस प्रगतिशील फैसले को बाद में मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम द्वारा कम कर दिया गया, ऐसा कहा गया था कि एक मुस्लिम महिला तलाक के बाद केवल 90 दिनों के 'इद्दत' के दौरान भरण-पोषण की मांग की जा सकती है.
2001 में, सुप्रीम कोर्ट ने 1986 अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा लेकिन स्पष्ट किया कि, एक पुरुष का अपनी तलाकशुदा पत्नी को बनाए रखने का दायित्व तब तक है जब तक कि महिला पुनर्विवाह नहीं कर लेती या खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ नहीं हो जाती.
नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तलाकशुदा महिलाओं के धर्म की परवाह किए बिना सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ता मांगने के अधिकार को मजबूत करता है.