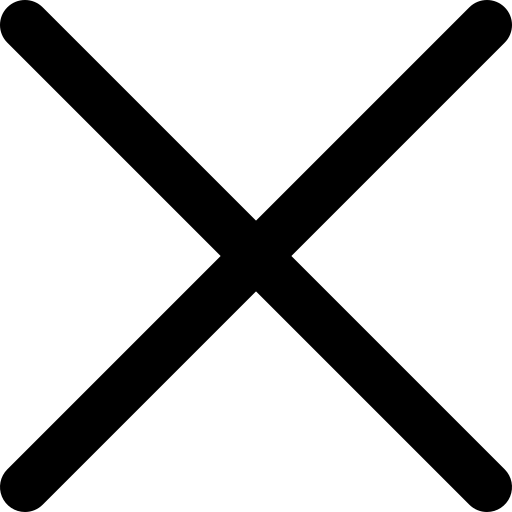पंकज सरन
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रेसीडेंसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली अमेरिका यात्रा है, जिसका समयकाल सटीक है. अगले एक साल में दोनों देश चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके होंगे और घरेलू मामलों में व्यस्त हा जाएंगे. 2019 के बाद से किसी भी दिशा में शिखर स्तर पर इस तरह की द्विपक्षीय यात्रा की अनुपस्थिति के बावजूद, रिश्ते ने इस अंतराल में कई सफलताएं देखी हैं, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समय के साथ रिश्ते में आई उछाल और गति की बात करती है.
ऐतिहासिक रूप से कहें, तो इस संबंध को निभाना आसान नहीं रहा है और ऐसा क्यों था, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है. 1985 में राजीव गांधी की रीगन के साथ व्हाइट हाउस की बर्फ तोड़ने वाली यात्रा के बाद से, यह संबंध प्रत्येक देश के भीतर विभिन्न राजनीतिक संरेखण के तनाव परीक्षण के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर कई संकटों से गुजरा है.
यह कहना शायद सच है कि रिश्ता अंततः परिपक्व होता दिख रहा है. फिर भी, जैसा कि अमेरिकी रणनीतिक साहित्य में हालिया लेखन से पता चलता है कि दोनों देश ‘आपसी अविश्वास के जाल’ से उबर चुके हैं, लेकिन अब वे ‘आपसी अपेक्षाओं के जाल’ में फंसते दिख रहे हैं. डिपलोमैट पीएस राघवन ने हाल ही में टिप्पणी की है कि ऐसा बेमेल संबंध ‘भारत-अमेरिका संबंधों में क्षमताओं और हितों की स्पष्ट विषमता’ से उत्पन्न होता है, जिसे पहचानना आवश्यक है.
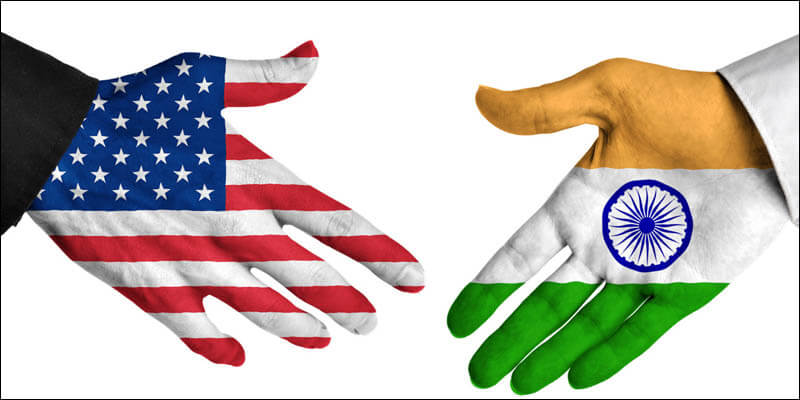
गौरतलब है कि हमें रिश्ते को ‘चीनी जाल’ में फंसने से रोकना चाहिए. सबसे पहली बात तो यह है कि चीन का खतरा इतना स्पष्ट होने से पहले ही संबंध उच्च स्तर पर आ गए थे. दूसरे, यदि आज चीन, अमेरिकी दृष्टिकोण में बड़ा है, जैसा कि उसकी नवीनतम राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में स्पष्ट है, तो यह समझने के लिए थोड़ी कल्पना की आवश्यकता है कि भारत की रणनीतिक गणना में चीन कितना बड़ा है.
भारत के लिए चीन तात्कालिक, स्पष्ट और वास्तविक है. यदि अमेरिका चीन के साथ सहयोग और प्रतिस्पर्धा की बात करता है और एक नए शीत युद्ध को रोकने की बात करता है, तो चीन के साथ रास्ता तलाशने में भारत की हिस्सेदारी और भी बड़ी है. चीन जैसे पड़ोसी के साथ निरंतर शत्रुता की स्थिति में रहने की संभावना वांछनीय नहीं है.
इन्हीं कारणों से भारत, अमेरिका में चीन के प्रति दृष्टिकोण संबंधी राष्ट्रीय सुरक्षा बहस पर करीब से नजर रख रहा है. अमेरिका और यूरोप के बीच और यूरोप के भीतर चीन से कैसे निपटा जा रहा है, इस पर भारत समान रूप से नजर रख रहा है.
तीसरे, अगर भारत-अमेरिका संबंध को अंतरराष्ट्रीय राजनीति के उतार-चढ़ाव के बावजूद बनाए रखना है, तो यह उद्देष्य चीन से बड़ा है और होना ही चाहिए. इस पर विश्वास करना आकर्षक और समीचीन है, लेकिन चीन वह गोंद नहीं हो सकता, जो रिश्ते को जोड़े रखता है.
न ही लोकतंत्र, स्वतंत्रता, बहुलवाद, विविधता और व्यक्ति की प्रधानता के हमारे साझा मूल्य विरोधाभासी हो सकते हैं. यदि ऐसा होता, तो दोनों देश वर्षों पहले ही गठबंधन साझेदार हो गए होते. इतिहास हमें सिखाता है कि रिश्ते के विकास के लिए ये मूल्य न तो आवश्यक हैं और न ही पर्याप्त हैं.
वे रिश्ते के लिए सर्वोत्तम अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं. अतीत में अमेरिका की कुछ निकटतम साझेदारियों पर नजर डालने से साझा मूल्यों की वितरणशीलता का पता चलेगा. भारत-अमेरिका साझेदारी कई परस्पर संबंधित कारकों से अपना अस्तित्व और स्थायित्व प्राप्त करती है, जो रिश्ते के लिए अंतर्जात और बहिर्जात दोनों हैं.

ये भी पढ़ें : देखें वीडियो: डा. अल-इस्सा के वक्तव्य पर आवाज द वाॅयस से क्या बोलीं देश की नामचीन हस्तियां
द्विपक्षीय रूप से, दोनों देशों के बीच पूरकता बढ़ रही है, जो एक-दूसरे की ताकत को मजबूत कर सकती है, चाहे वह आर्थिक, रक्षा या रणनीतिक क्षेत्र में हो. हमारे लोगों की भलाई और कल्याण को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों पर हमारे सहयोग को गहरा करके दीर्घकालिक संबंध का आधार बनने की जरूरत है. अमेरिका के साथ अच्छे संबंध होने से भारत के उत्थान में मदद मिलेगी.
यह दोहराया जाना चाहिए कि भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह उच्च प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण कच्चे माल, ऊर्जा और बड़े बाजारों के सही वैश्विक स्रोतों के साथ कितना एकीकृत होता है और अपनी ताकत बनाने के लिए इस तरह के एकीकरण का लाभ कैसे उठाता है.
भारत के आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योग की सफलता का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी उद्योगों के कारण है, लेकिन समय के साथ यह अमेरिकी कॉरपोरेट्स के लिए एक प्रमुख शक्ति गुणक बन गया है. दूसरी ओर, अपनी राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में भारत की सफलता, यह साबित करना कि लोकतंत्र काम करता है और यह सुनिश्चित करना कि 1945 के बाद की विश्व व्यवस्था से कठोर बदलाव व्यवस्थित हो, ये सभी अमेरिका के हित में हैं.
ये भी पढ़ें : नफरत के सिद्धांतों ने Radicalism and Terrorism बढ़ायाः Dr. Al-Issa
वैश्विक स्तर पर, मौजूदा शक्तियों को चुनौती दी जा रही है, नई शक्तियाँ उभर रही हैं, जबकि अन्य घट रही हैं. जिस तरह अमेरिका एक उभरते हुए चीन और एक कमजोर रूस को देख रहा है, उसी तरह एक उभरता हुआ भारत एक उभरती हुई वास्तविकता है.
भारत का परिवर्तन, अमेरिका के लिए भारत के परिवर्तन की दिशा और गति को प्रभावित करने का एक अवसर है. इसके लिए एक नवोन्मेषी दृष्टिकोण और भारत के बारे में अधिक सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होगी. अमेरिका को भारत से गठबंधन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.
उसे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्वीकार करने और उससे इस तरह व्यवहार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो समय के साथ अपनी सभ्यतागत पहचान पर जोर देगा. दूसरी ओर, भारत को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अमेरिका उसकी सभी समस्याओं का समाधान होगा.
बड़े रणनीतिक दृष्टिकोण से, यह उभरते हुए भारत का अमेरिका के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था में फिट होने का द्वंद्व है, जो आगे बढ़ने पर रिश्ते की अंतर्निहित धारा का निर्माण करेगा.
एक अमेरिका है, जो अपनी बेलगाम शक्ति को चुनौती दिए जाने की संभावना देख रहा है और एक उभरता हुआ भारत है, जो दुनिया में अपनी जगह फिर से हासिल करना चाहता है, यह स्थिति संभावित रूप से सहयोग के लिए अपार अवसर प्रदान कर सकती है. इसकी सफलता रणनीतिक अभिसरण और आपसी विश्वास की सीमा पर निर्भर करेगी, क्योंकि वे परिवर्तन को आगे बढ़ाते हैं और नेतृत्व करते हैं. यह एक गतिशील एवं समय के प्रति संवेदनशील प्रक्रिया है.
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बार-बार इस समय को ‘अमेरिका और दुनिया के लिए निर्णायक दशक’ के रूप में वर्णित करती है.
राष्ट्रों के व्यापक समुदाय के लिए जो बात दांव पर है, वह भारत और अमेरिका जैसे लोकतंत्रों की, न केवल अपनी आंतरिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता है, बल्कि ‘वैश्विक दक्षिण’ के देशों के विकास के लिए उनकी आशा और सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सहायता प्रदान करने की उनकी क्षमता भी है.
दोनों पक्षों ने अब तक रूस पर अपने मतभेदों को उम्मीद से ज्यादा बेहतर तरीके से प्रबंधित किया है. यह एक अच्छा संकेत है. हालाँकि समस्या दूर नहीं हुई है और इसकी संभावना भी नहीं है. रूस, अमेरिका के लिए ‘अंध स्थान’ बना रहेगा. भारत, रूस और चीन को एक ही नजरिए से देखने का जोखिम नहीं उठा सकता. शायद रिश्ते का सबसे कठिन हिस्सा, इसकी द्विपक्षीय सीमाओं के बाहर हो सकता है.
ये भी पढ़ें : India में कोई भी Religion खतरे में नहींः Ajit Doval