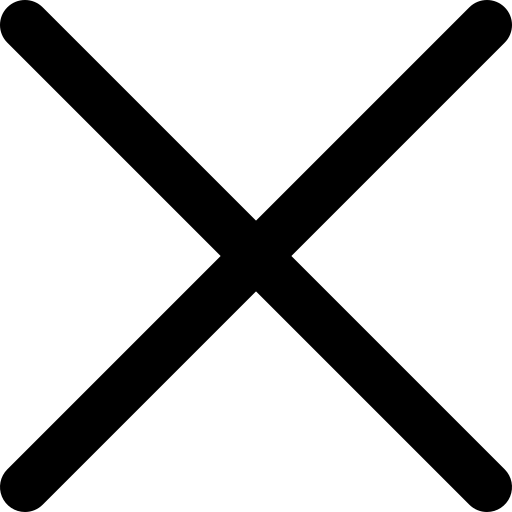प्रमोद जोशी
प्रमोद जोशी
इस महीने 14 मई को तुर्की में होने वाले संसदीय और राष्ट्रपति पद के चुनाव पर दुनिया की निगाहें हैं. तुर्की की आंतरिक स्थिति और विदेश-नीति दोनों लिहाज से ये चुनाव महत्वपूर्ण होंगे. सबसे बड़ा सवाल राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के भविष्य को लेकर है. चुनाव-पूर्व सर्वेक्षणों से लगता है कि वे हार भी सकते हैं.
एर्दोगान की हार या जीत से तुर्की की आंतरिक और विदेश-नीति दोनों प्रभावित होंगी. अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया के देशों, यहाँ तक कि भारत के साथ रिश्तों पर भी इनका असर होगा. सत्ता परिवर्तन हुआ, तो बदलाव भी होंगे, पर उनमें समय लगेगा.
मसलन यदि देश संसदीय-प्रणाली की ओर वापस ले जाने का प्रयास किया जाएगा, तो उसे पूरा होने में समय लगेगा. इस लिहाज से केवल राष्ट्रपति पद के चुनाव का ही नहीं साथ में हो रहे संसदीय चुनावों का भी महत्व है.
एर्दोगान-विरोधी मोर्चा
देश के छह विरोधी दलों ने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया है और राष्ट्रपति पद के लिए एर्दोगान के खिलाफ पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी (सीएचपी) के कमाल किलिचदारोग्लू को अपना प्रत्याशी बनाया है. उन्हें कुर्द-पार्टी एचडीपी का भी समर्थन हासिल है.
आरोप है कि एर्दोगान के नेतृत्व में तुर्की की व्यवस्था निरंकुश होती जा रही है. देश में जबर्दस्त वैचारिक ध्रुवीकरण है. इस प्रवृत्ति को विपक्ष रोकना चाहता है. एर्दोगान विरोधी मोर्चे की घोषणा है कि यदि हम जीते तो यूरोपियन यूनियन की सदस्यता हासिल करने की कोशिश करेंगे और अमेरिका का जो भरोसा खोया है, उसे वापस लाएंगे.
मुद्रास्फीति की दर अगले दो साल में दस फीसदी के अंदर लाने की कोशिश करेंगे और सीरिया से आए करीब 36 लाख शरणार्थियों को उनकी सहमति से वापस भेजेंगे. तुर्की नेटो का सदस्य है, पर यूक्रेन के युद्ध के कारण उसके अंतर्विरोध हाल में उभरे हैं.
हाल में उसकी नीतियों में कुछ बदलाव भी आया है. उसने नेटो में फिनलैंड की सदस्यता को रोक रखा था, जिसकी स्वीकृति अब दे दी. नेटो में नई सदस्यता के लिए सर्वानुमति जरूरी होती है.
विदेश-नीति
हालांकि एर्दोगान ने अपनी विदेश-नीति को लेकर पश्चिमी देशों की अनदेखी की है, पर जिन कंपनियों पर पश्चिमी देशों ने पाबंदियाँ लगाई हैं, उन्हें रूस के साथ कारोबार करने की अनुमति भी नहीं दी है. अब वह पश्चिमी निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश भी कर रहा है.
दो राय नहीं कि इस समय ईयू और अमेरिका के साथ तुर्की के रिश्ते सबसे खराब दौर में हैं. उसने रूस से एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद कर अमेरिका से नाराजगी मोल ले रखी है. दूसरी तरफ सीरिया में कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल है.
एर्दोगान मानते हैं कि 2016 में उनके खिलाफ बगावत के पीछे अमेरिका का हाथ था. इसके अलावा सायप्रस और ग्रीस के साथ सामरिक टकराव और सीमा-विवाद भी इस मतभेद के पीछे है. यदि उनके विरोधी सत्ता में आए, तो बेशक पश्चिमी देशों के साथ इन मसलों पर टकराव कम होगा.
अर्थव्यवस्था
एर्दोगान-विरोधी यदि सत्ता में आए, तो दो काम वे फौरन करेंगे. एक तो अर्थव्यवस्था को काबू में करने की कोशिश करेंगे और दूसरे बड़ी संख्या में राजनीतिक बंदियों को रिहा करेंगे. ये दोनों बातें अमेरिका और पश्चिमी देशों के मन की हैं. इससे तुर्की को ईयू में शामिल करने की बातचीत फिर से शुरू होगी. इसके अलावा स्वीडन की नेटो सदस्यता के रास्ते में बाधाएं भी दूर होंगी.
बावजूद इसके तुर्की के रूस से रिश्ते बने रहेंगे, क्योंकि किलिचदारोग्लू सरकार रूस के खिलाफ पाबंदियों का बहुत समर्थन नहीं करेगी और यूक्रेन मामले में वह तटस्थता की नीति अपनाएगी. तुर्की की राजनीति में आम धारणा है कि अमेरिका इस क्षेत्र में हमेशा प्रभावशाली नहीं रहेगा, इसलिए रूस से दुश्मनी लेने का कोई मतलब नहीं है. पर एस-400 एयर डिफेंस को नई व्यवस्था खारिज करना चाहेगी.
एर्दोगान विरोधियों को कुर्दों का समर्थन प्राप्त है, पर वे उत्तरी सीरिया के कुर्दों के साथ फौरन समझौता करने की स्थिति में नहीं होंगे और न उस क्षेत्र से तुर्की की सेना की वापसी होगी. अलबत्ता सीरिया की बशर अल असद सरकार के साथ बात करके 36 लाख शरणार्थियों को वापस भेजने की कोशिश होगी. शायद उसके बाद सीरिया से सेना वापस बुलाने पर चर्चा हो. अलबत्ता इसमें समय लगेगा.
भारत से रिश्ते
एर्दोगान के दौर में तुर्की और भारत के रिश्ते खराब होते गए हैं. सरकार बदली, तो वे पहले से बेहतर होंगे. इस साल फरवरी में आए भूकंप के बाद भारत ने ‘ऑपरेशन दोस्त’ के तहत फौरन सहायता पहुँचाई थी, जिससे माहौल बेहतर हुआ है.
भारत की स्वतंत्रता के समय तुर्की के साथ हमारे रिश्ते बेहतर थे. अतातुर्क कमाल पाशा का तुर्की ऐसा मुस्लिम देश था, जो धर्मनिरपेक्ष भी था. दूसरी तरफ 1952 में वह नेटो का सदस्य बन गया, जबकि भारत ने गुट-निरपेक्षता का रास्ता पकड़ा. शीतयुद्ध के दौर में भारत और तुर्की की दूरी बढ़ती चली गई. इस दौरान तुर्की और पाकिस्तान दोस्त बनते चले गए.1965 और 1971 की लड़ाइयों में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की.
कश्मीर का काँटा
1974 में तुर्की ने जब सायप्रस पर हमला किया तो भारत ने सायप्रस का साथ दिया. पाकिस्तान ने तुर्की का समर्थन किया था. उधर ओआईसी के स्थायी एजेंडा में फलस्तीन और कश्मीर दो सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं, जो भावनात्मक रूप से इस्लामी देशों को छूते हैं.
1994 मे ओआईसी में कश्मीर पर विशेष कांटैक्ट ग्रुप के बन जाने के बाद तुर्की और भारत के रिश्तों में और दरार पैदा हुई. इस कांटैक्ट ग्रुप में तुर्की, अजरबैजान, नाइजर, पाकिस्तान और सउदी अरब सदस्य हैं. बावजूद इसके दोनों देशों के शासनाध्यक्षों का एक-दूसरे के यहाँ आना-जाना चलता रहा.
1974 से 2002 तक चार बार प्रधानमंत्री बने मुस्तफा बुलंट येविट (या एक्याविट) भारत का आदर करते थे. उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता और गीतांजली का अपनी भाषा में अनुवाद भी किया था. 2002 में एर्दोगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी इस्लाम के नाम पर सत्ता में आई. उसके बाद से तुर्की के दृष्टिकोण में काफी बदलाव आया है.
एर्दोगान तुर्की को मुस्लिम देशों के नेता और क्षेत्रीय शक्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इससे उनके सामने दिक्कतें भी पैदा हुई हैं. भारत के साथ तुर्की के रिश्तों में जो खलिश है, उसके पीछे कारोबारी और तकनीकी कारण भी हैं. भारत की पश्चिम एशिया-नीति से भी वह असहमत है.
एर्दोगान की सत्ता
राष्ट्रपति एर्दोगान पिछले बीस साल से ज्यादा समय से सत्ता पर आसीन है. 2003 से 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में और उसके बाद राष्ट्रपति के रूप में. उनकी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी (एके पार्टी) का आधार इस्लाम में है, जो नवंबर 2002 से सत्ता में है. राष्ट्रवादी पार्टी एमएचपी का एर्दोगान के साथ गठबंधन है. 2016 में हुई एक बगावत का एर्दोगान ने कठोर हाथों से दमन किया था, जिसकी कड़वाहट राजनीति में मौजूद है.
देश का मीडिया काफी हद तक एर्दोगान समर्थकों के हाथों में है. इस समय एर्दोगान सबसे जबर्दस्त विरोध का सामना कर रहे हैं. देश में कट्टरपंथ और उदारवाद के बीच मुकाबला है. इस साल फरवरी में आए भूकंप के बाद एकबारगी लगा था कि शायद चुनाव टल जाएं, पर गत 10 मार्च को एर्दोगान ने समय से पहले चुनाव की घोषणा कर दी.
देश में महंगाई चरम पर है. मुद्रास्फीति की दर आधिकारिक तौर पर 50 प्रतिशत के आसपास है, पर स्वतंत्र अर्थशास्त्री मानते हैं कि यह 100 प्रतिशत से भी ज्यादा है.
शासन-प्रणाली
विरोधी दलों का गठबंधन एर्दोगान द्वारा स्थापित अध्यक्षात्मक प्रणाली से संसदीय प्रणाली में वापस लाना चाहता है. इसके लिए संसद के 600 में से 400 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी. यदि वे इस विषय पर राष्ट्रीय जनमत-संग्रह कराना चाहेंगे, तो उसके लिए भी उन्हें 360 सांसदों की जरूरत होगी.
चूंकि राष्ट्रपति पद के साथ संसद के चुनाव भी हो रहे हैं, इसलिए उसके परिणाम पर भी नजरें रखनी होंगी. तुर्की में मतदान आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है. यानी कि पार्टियाँ अपने प्रत्याशियों की सूची घोषित करती हैं.
तुर्की और विदेश में रहने वाले करीब साढ़े छह करोड़ मतदाता इस मतदान में शामिल हो रहे हैं. मतदाता किसी प्रत्याशी को नहीं, बल्कि पार्टी को वोट देते हैं. पार्टी को मिले अनुपात के आधार पर उसके प्रत्याशी संसद के सदस्य बनते हैं.
एर्दोगान द्वारा बनाई गई व्यवस्था के अनुसार अब सरकार का गठन राष्ट्रपति करते हैं. देश में प्रधानमंत्री नहीं होता. वर्तमान संसद में एर्दोगान समर्थक पीपुल्स एलायंस की संख्या 334 है.
चुनाव-प्रणाली
राष्ट्रपति पद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव 2014 में आयोजित किया गया था. उसके पहले 2007 में एक जनमत संग्रह के बाद पिछली प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष को विधायिका, तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली द्वारा चुना जाता था.
नई व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति के चुनाव 2012 में होने थे, पर जब 2012 में चुनाव का मौका आया, तब तय किया गया कि 2014 में होंगे. राष्ट्रपति अधिकतम दो बार पांच साल की अवधि तक काम कर सकते हैं. यदि दूसरे कार्यकाल की समाप्ति से पहले मध्यावधि चुनाव होते हैं, तो उन्हें तीसरे कार्यकाल की अनुमति दी जा सकती है.
एर्दोगान चूंकि दो बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, इसलिए उनका तीसरी बार चुनाव लड़ना असंवैधानिक होना चाहिए, पर देश के चुनाव आयोग वाईएसके ने व्यवस्था दी है कि उनका पहला कार्यकाल 2014 से नहीं, 2018 से गिना जाएगा, जब राष्ट्रपति और संसद के चुनाव पहली बार एकसाथ हुए थे.
राष्ट्रपति पद का चुनाव दो दौर में होता है. पहले स्तर पर यदि कोई उम्मीदवार साधारण बहुमत यानी 50 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त नहीं करता, तो पहले दौर के दो सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवारों के बीच पुनः मुकाबला होता है, जिसके बाद विजेता को निर्वाचित घोषित किया जाता है.
( लेखक दैनिक हिन्दुस्तान के संपादक रहे हैं )