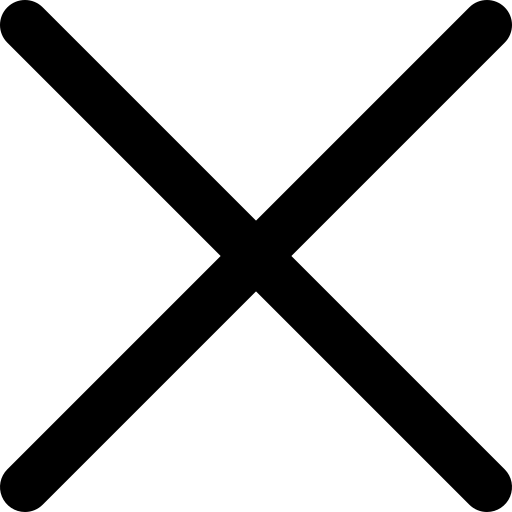प्रमोद जोशी
पहलगाम-हमले के बाद पाकिस्तान को सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि हम कश्मीर में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाकर रखें. दुनिया का अनुभव है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लंबी चलती है. सवाल है कि इस आतंकी हमले की योजना क्यों बनाई गई और यही समय क्यों चुना गया?
फिलहाल कश्मीर में सबसे बड़ी ज़रूरत वहाँ के निवासियों का भरोसा जीतने की और पाकिस्तानी हरकतों का जवाब देने की है. सीमा पार से एटम बम दागने की धमकियाँ दी जा रही हैं. हमें ऐसी रणनीति बनानी होगी, जो कम से कम जोखिम उठाकर पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा बड़ी सज़ा दे सके.
हालात जिस मोड़ पर आ गए हैं, उसमें भारत को कार्रवाई करनी ही होगी. पानी रोकने के अलावा हमारे पास आतंकी केंद्रों पर हमले का विकल्प भी है. सरकार के एक शीर्ष सूत्र ने दिल्ली के एक राष्ट्रीय दैनिक से कहा है कि सैनिक कार्रवाई होगी. हम तैयार हैं और हमले के तरीके पर चर्चा कर रहे हैं.
सवाल है कि क्या हमारी सेना एलओसी पार करके पीओके में प्रवेश कर सकती है? क्या नौसेना कराची बंदरगाह की नाकेबंदी करेगी? एलओसी पर गोलाबारी रोकने को लेकर 2021में जो समझौता हुआ था, वह भी अब टूटता हुआ लग रहा है.सबसे बड़ा खतरा बैक-चैनल संपर्क टूटने का है. इसे टूटना नहीं चाहिए और उन्मादी बयानों से बचना भी चाहिए.
राजनयिक उपाय
भारत ने सिंधु जल संधि को ‘स्थगित’ करने के अलावा कुछ दूसरे राजनयिक उपायों की घोषणा की है. वहीं पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित करने का फैसला किया है, जिनमें शिमला समझौता शामिल है.
पानी, हवा और जलवायु ऐसी प्राकृतिक निधियाँ हैं, जिनका समझदारी और सहयोग के साथ इस्तेमाल अच्छे पड़ोस की निशानी है, पर ‘आतंकवादी गतिविधियाँ’ इन मूल्यों पर पानी फेरती हैं.
पहली नज़र में ये फैसले प्रतीकात्मक हैं और इनका असर बहुत सीमित होगा. शिमला-समझौता काफी पहले भंग हो चुका है और आज उसका कोई मतलब नहीं है, पर सिंधु-संधि जीवित सच्चाई है. सिंधु का पानी रुका, तो पाकिस्तान में तबाही मचेगी.
सिंधु का पानी रोके जाने से जुड़े तमाम किंतु-परंतु भी हैं. पानी रोकना व्यावहारिक-दृष्टि से आसान नहीं है, दूसरे पाकिस्तानी नेता धमकियाँ दे रहे हैं कि पानी रुका, तो हम इसे युद्ध की घोषणा मानेंगे. हमारे पास एटम बम है.
उन्हें लगता है कि एटम बम रामबाण है. वे इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि भारत के पास भी एटम बम है और एकबार बम चलने का मतलब है, बड़े स्तर पर विध्वंस.
एटमी धमकी
एटम बम के मामले में पाकिस्तान ‘नो फर्स्ट यूज़’ की नीति को नहीं मानता. भारत मानता है कि हम पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर इस नीति में बदलाव की बातें भी हैं.
अगस्त 2019 में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था, ''अभी तक हमारी नीति है कि हम परमाणु हथियार का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन भविष्य में यह नीति हालात पर निर्भर करेगी.'' इससे पहले 2016में मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि भारत इस नीति से बँधा नहीं रह सकता.
ज्यादा बड़ा सवाल है कि क्या भारत सिंधु का पानी रोक पाएगा, क्योंकि पानी रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. क्या संधि की व्यवस्थाएँ भारत को पानी रोकने देंगी? क्या पाकिस्तान इस मामले को अंतरराष्ट्रीय फोरमों पर चुनौती नहीं देगा?
सिंधु जल
भारतीय संसद की एक कमेटी ने 2021 में सुझाव दिया था कि इस संधि की व्यवस्थाओं पर फिर से विचार करने और संशोधन करने की जरूरत है. उससे पहले जम्मू-कश्मीर विधानसभा भी इस आशय के प्रस्ताव पास कर चुकी थी.
दोनों देशों के बीच सितंबर, 1960 में सिंधु जल संधि विश्वबैंक की मध्यस्थता में हुई थी. इसमें तीन पश्चिमी नदियाँ—सिंधु, झेलम और चेनाब और तीन पूर्वी नदियाँ-सतलुज, ब्यास और रावी शामिल हैं. संधि के अनुसार पूर्वी नदियों के पानी का भारत पूरी तरह इस्तेमाल कर सकता है.
पश्चिमी नदियाँ पाकिस्तान को आवंटित की गई हैं, लेकिन भारत के पास घरेलू उपयोग, सिंचाई और पनबिजली उत्पादन सहित पानी के ‘गैर-उपभोग’ के सीमित अधिकार हैं.
पाकिस्तान की 80 फीसदी से ज़्यादा खेती और लगभग एक तिहाई पनबिजली सिंधु के पानी पर निर्भर है. संधि स्थगित होने का मतलब यह भी नहीं है कि अगले ही दिन पानी रोक दिया जाएगा. व्यावहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं है.
भारत के पास पश्चिमी नदियों के अरबों क्यूबिक मीटर पानी को रोकने के लिए विशाल भंडारण भले ही नहीं है. पर कुछ वर्षों में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन भी सकता है.
अलबत्ता भारत अब नदी से जुड़ा हाइड्रोलॉजिकल डेटा और प्रवाह में अचानक आने वाले बदलाव की पूर्व सूचना पाकिस्तान को नहीं देगा. दूसरे अपनी तरफ ऐसे बाँध और नहरें बनाने को स्वतंत्र होगा, जिनसे पानी का स्थानीय भंडारण या उपभोग संभव हो.

हम क्या करेंगे ?
ये कुछ दूर की बातें हैं, फिलहाल अपने मौजूदा बुनियादी ढाँचे का उपयोग करके भारत, जल-प्रवाह को आंशिक रूप से भी नियंत्रित कर पाया, तो पाकिस्तान को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. खासकर गर्मियों में जब पानी की जरूरत ज्यादा होती है.
बरसात में बिना किसी पूर्व चेतावनी के अचानक बड़ी मात्रा में पानी आने पर डाउनस्ट्रीम में काफी नुकसान का खतरा भी होगा. रविवार को पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि भारत ने अनंतनाग क्षेत्र से झेलम नदी में अचानक पानी छोड़ा है, जिसकी पूर्व-सूचना नहीं दी. इससे मुज़फ़्फ़राबाद और हट्टियन बाला के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है.
सिंधु जल संधि के बाद, भारत ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई और पनबिजली के लिए रावी, ब्यास और सतलुज से अपने 33मिलियन एकड़ फुट (एमएएफ) हिस्से का प्रभावी दोहन किया. सतलुज पर भाखड़ा, ब्यास पर पोंग और रावी पर रंजीत सागर बाँध जैसे बुनियादी ढाँचे ने भारत को अपने आवंटित हिस्से का लगभग 95प्रतिशत उपयोग करने में समर्थ बना दिया.
परियोजनाओं में तेज़ी
पश्चिमी नदियों पर भारत का उपयोग न्यूनतम रहा है, जो बगलिहार, सलाल और किशनगंगा परियोजनाओं के रूप में हैं. पिछले कुछ वर्षों में विवाद बढ़ने के बाद से इस काम में अब तेजी आ गई है.
पिछले हफ्ते शुक्रवार को हुई बैठक में चेनाब पर चल रही पनबिजली परियोजनाओं पर तेजी से काम करने पर चर्चा हुई. किश्तवाड़ जिले में 850मैगावाट रतले, 1,000मैगावाट पाकल दुल, 624मैगावाट किरू और 540मैगावाट क्वार पर काम विभिन्न चरणों में है.
ऊर्जा मंत्रालय को चार प्रस्तावित परियोजनाओं पर भी काम में तेजी लाने के लिए कहा गया है. इनमें 1,856मैगावाट की सावलकोट, 930मैगावाट की किरथाई-2, 260मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज-2और 240मैगावाट की उड़ी-1स्टेज-2शामिल हैं.
ये परियोजनाएँ पाकिस्तान में नदियों के प्रवाह को बाधित नहीं करती हैं, फिर भी इन बाँधों के डिजाइन को लेकर पाकिस्तान की आपत्तियाँ हैं, जिनकी वजह से 2010से दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है.
भारत अब सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी का बेहतर उपयोग करने के लिए चेनाब से रावी तक पानी स्थानांतरित करने के लिए 10-12किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने पर विचार भी कर रहा है.

पाकिस्तान में संकट
हिमालय की नदियों में अपार जलविद्युत क्षमता है, जो अनुमानतः एक लाख 50हजार मैगावाट से अधिक है. सच यह भी है कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ इस क्षमता के दोहन का अतीत में खास प्रयास नहीं किया.
सिंधु जल संधि में भारत के रुख के कारण, पाकिस्तान अब दोहरे संकट में आ गया है, जिसका परिणाम है, चोलिस्तान परियोजना का स्थगन. चोलिस्तान परियोजना में छह नहरों का निर्माण होना है. पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में दो-दो नहरें, जिनसे लाखों एकड़ रेगिस्तानी भूमि की सिंचाई होगी. इनमें पाँच नहरें सिंधु नदी से और छठी सतलुज से पानी लेगी.
ग्रीन पाकिस्तान इनीशिएटिव के तहत यह पाकिस्तानी सेना समर्थित परियोजना है, जिसे फरवरी में सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर और पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने लॉन्च किया था.
परियोजना के शुरू होने से आक्रोश और विरोध भी भड़का है, खासतौर से सिंध में, जो पानी की लगातार कमी से जूझ रहा है. सिंध विधानसभा ने मार्च में एक प्रस्ताव पारित किया और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर विनाशकारी परिणामों की चेतावनी दी.
पाकिस्तानी रणनीति
जिस समय यह संधि हुई थी उस समय 1947के कश्मीर-प्रकरण के अलावा पाकिस्तान के साथ भारत का कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था. संधि के तीन साल बाद ही 1963में पाकिस्तान ने कश्मीर की 5,189किमी जमीन चीन को सौंपी, जिसके बाद उसकी रणनीति में बदलाव आया.
पाकिस्तानी रणनीति की परिणति 1965में कश्मीर पर हुए हमले के रूप में दिखाई पड़ी. तबसे पाकिस्तान लगातार भारत के साथ हिंसा के विकल्प तलाशने लगा है.
आतंकवादी घटनाएं बढ़ने पर भारत ने पानी के इस्तेमाल पर विचार करना शुरू किया और अपने हिस्से के पानी का पूरा सदुपयोग करने के लिए जलविद्युत परियोजनाएं शुरू कीं, ताकि संधि के दायरे में रहते हुए भारत ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर सके.
पाकिस्तानी राजनेता और मीडिया नरेंद्र मोदी के सितंबर 2016के एक बयान का उल्लेख करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता. यह बयान उड़ी पर हुए हमले के बाद दिया गया था.
विवाद की शुरुआत
मोदी का आशय जो भी रहा हो, पर पाकिस्तान ने उस बयान के छह साल पहले 2010में ही अंतरराष्ट्रीय फोरम पर इस विवाद को उठा दिया था. इसकी एक वजह अपने देश की आंतरिक राजनीति में यह साबित करना था कि देश में पानी का संकट भारत की वजह से है. प्रधानमंत्री मोदी के बयान से उसे आड़ मिल गई.
पाकिस्तान की शिकायतें 2006के आसपास शुरू हो गई थीं, जब भारत ने इन नदियों पर पनबिजली परियोजनाएं बनाईं. मई, 2010में पाकिस्तान ने किशनगंगा और बगलिहार परियोजनाओं को लेकर हेग में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के सामने यह मसला रखा.
पाकिस्तान का कहना था कि भारत को इन नदियों पर बाँध बनाकर बिजली बनाने का अधिकार है ही नहीं, इसलिए किशनगंगा बाँध का निर्माण रोका जाए. दिसंबर 2013में कोर्ट के फैसले में कहा गया कि भारत के निर्माण को रोका नहीं जा सकता, अलबत्ता भारत को ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान को न्यूनतम 9क्यूमैक्स (क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड) पानी मिलता रहे.
भारत को शिकायत है कि संधि के अंतर्गत विवादों के निपटारे के लिए दोनों सरकारों के बीच बनी व्यवस्था की पाकिस्तान ने अनदेखी की है. विवादों के निपटारे के लिए संधि के अनुच्छेद 9में जो चरणबद्ध व्यवस्था की गई थी, उसे पाकिस्तान ने तोड़ दिया.
जब गतिरोध नहीं टूटा, तो भारत ने 2023में संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत इस्लामाबाद को एक औपचारिक नोटिस जारी किया, जिसमें पहली बार संधि में संशोधन की माँग की गई.

शिमला समझौता
पाकिस्तान ने सिंधु संधि पर भारतीय फैसले के जवाब में शिमला समझौते को स्थगित करने की घोषणा की है. यह समझौता कश्मीर मामले के ‘अंतरराष्ट्रीयकरण’ को रोकता है.
इस बात का अब कोई मतलब रह नहीं गया है, क्योंकि पाकिस्तान इस समझौते पर दस्तखत करने के बावज़ूद वर्षों से संयुक्त राष्ट्र महासभा या दूसरे अंतरराष्ट्रीय फोरमों में कश्मीर मामले को उठाता रहा है.
1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद 1972में हुआ यह समझौता मुख्य रूप से दो बातों से संबंधित है: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का संचालन कैसे किया जाएगा, और नियंत्रण रेखा (एलओसी) को वास्तविक सीमा के रूप में मान्यता देना.
पाकिस्तान को उस समय अपने 93,000 युद्धबंदियों की रिहाई की फिक्र थी. भारत चाहता था कि इस बहाने एलओसी पर स्थिरता कायम हो जाने के बाद कश्मीर समस्या के स्थायी समाधान का रास्ता खुल जाएगा.
समझौते में कहा गया है कि समस्या का अंतिम समाधान होने तक, दोनों में से कोई भी पक्ष एकतरफा तरीके से स्थिति में बदलाव नहीं करेगा. इसके बावज़ूद पाकिस्तान ने कभी इसका पालन नहीं किया. 1999में करगिल हमला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है.
2019के बाद, जब भारत ने अनुच्छेद 370को निरस्त किया, तब पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत ने समझौते का उल्लंघन किया है. हालांकि यह भारत की आंतरिक व्यवस्था थी, जिसमें पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का समझौता शामिल नहीं था.
(लेखक दैनिक हिन्दुस्तान के संपादक रहे हैं)