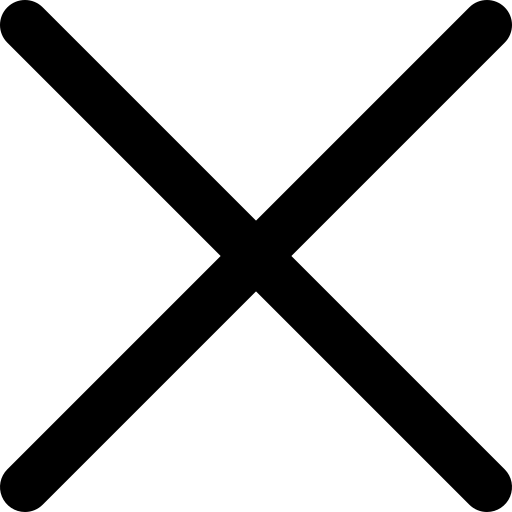आतिर खान
इस ईद पर, एक मुसलमान समुदाय को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकता है, वह है भविष्य के लिए एक नई मेटा-कथा बनाने के सामूहिक प्रयास में सक्रिय रूप से भाग लेना. ईद पारंपरिक रूप से युवा पीढ़ी को सार्थक उपहार देने का समय है.
आज हम जो सबसे प्रभावशाली उपहार दे सकते हैं, वह है जीवन जीने का एक नया तरीका - जो इस्लामी अध्ययन, सूफीवाद, तर्कवाद और सांस्कृतिक पहचान की मान्यता को मिलाता है, जो अंततः मुस्लिम समुदाय के लिए एक एकीकृत और प्रगतिशील भविष्य की कल्पना करता है.
इस्लाम के भीतर, इसकी स्थापना के बाद से ही तीन प्रमुख विचारधाराएँ सह-अस्तित्व में रही हैं: उलेमा (धार्मिक विद्वान), सूफीवाद (रहस्यवादी), और तर्कवादी (वे जो बौद्धिक और दार्शनिक जांच को अपनाते हैं). प्रत्येक ने मुस्लिम विचार के विकास में अद्वितीय योगदान दिया है.
हालाँकि, किसी एक विचारधारा पर अत्यधिक जोर, अक्सर दूसरों की कीमत पर, मुसलमानों के लिए एक प्रगतिशील और समग्र पहचान के विकास में बाधा उत्पन्न करता है.
ऐतिहासिक रूप से, इब्न रुश्द (एवर्रोस) जैसे लोगों ने विज्ञान और दर्शन दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, यूरोपीय ज्ञानोदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. फिर भी, इन योगदानों को अक्सर मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा अनदेखा किया जाता था या संदेह के साथ देखा जाता था, क्योंकि वे कुछ धार्मिक शिक्षाओं के साथ संघर्ष करते थे.
डर यह था कि ऐसे विचार इस्लामी मान्यताओं और प्रथाओं को कमजोर कर सकते हैं. उसी समय, सूफीवाद, अपने रहस्यवादी दृष्टिकोण के साथ, "मुख्यधारा" या "सही" इस्लामी परंपराओं के बाहर मानी जाने वाली प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए उलेमा की आलोचना का सामना कर रहा था.
'शिर्क' (अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ को ईश्वरीय गुणों का श्रेय देना) के आरोप आम थे. विभिन्न विचारधाराओं के बीच इन तनावों ने, समय के साथ, मुसलमानों को अपने समुदाय के लिए अधिक व्यापक और प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाने से रोका है.
हालाँकि, इन दृष्टिकोणों के बीच सामंजस्य महत्वपूर्ण है. इस्लाम केवल एक धर्म नहीं है; यह एक सामाजिक परियोजना, एक नैतिक ढांचा और एक विचारधारा है. यह समझना कि आस्था के लिए विभिन्न व्याख्याएँ और दृष्टिकोण मौजूद हैं, मुस्लिम प्रगति के लिए आवश्यक है.
आध्यात्मिक और व्यावहारिक के बीच संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है. मुसलमानों को न केवल परलोक (आखिरत) पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने का भी प्रयास करना चाहिए.
सार्थक वर्तमान की खोज परलोक की उपेक्षा की कीमत पर नहीं होनी चाहिए, और इसके विपरीत. केवल दोनों पहलुओं को अपनाने से ही मुसलमान आध्यात्मिक रूप से पूर्ण और व्यावहारिक रूप से अपने लिए, अपने परिवार और समाज के लिए समृद्ध जीवन जी सकते हैं.
जीवन के प्रति एक सक्रिय, संलग्न दृष्टिकोण - जो आस्था और कर्म के बीच संतुलन बनाता है - भाग्य पर निष्क्रिय निर्भरता से कहीं अधिक मूल्यवान है. दुर्भाग्य से, यह विश्वास कि सब कुछ पूर्वनिर्धारित है, एक महत्वपूर्ण बाधा बन गया है, खासकर भारत सहित मुस्लिम दुनिया के कुछ हिस्सों में. भारत में, धार्मिक विद्वान या उलेमा मुस्लिम समुदाय में एक प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं.
हालाँकि, अधिकांश शैक्षणिक प्रणाली पारंपरिक इस्लामी शिक्षाओं में डूबी हुई है, जो मुख्य रूप से कुरान, हदीस और न्यायशास्त्र पर केंद्रित है.जबकि कुछ विद्वान असाधारण हैं, अधिकांश संस्थानों में अपने पाठ्यक्रम को समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं के साथ संरेखित करने या आधुनिक शैक्षिक मानकों को पूरा करने की दृष्टि का अभाव है.
अधिकांश भारतीय मुसलमान इन संस्थानों से अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिनमें अक्सर धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए आधुनिक शोध-उन्मुख दृष्टिकोण का अभाव होता है.
यहाँ तक कि अल-अजहर जैसे विश्व-प्रसिद्ध इस्लामी संस्थानों को भी अपने पाठ्यक्रम को समकालीन मुद्दों के लिए प्रासंगिक बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.
शिक्षा में इस अंतर ने कई मुसलमानों की बौद्धिक और सामाजिक रूप से आधुनिक दुनिया से जुड़ने की क्षमता को सीमित कर दिया है. पारंपरिक इस्लामी शिक्षा के विपरीत, सूफीवाद का अभ्यास कई भारतीय मुसलमानों के लिए एक बहुत जरूरी आध्यात्मिक शरण प्रदान करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अजमेर शरीफ और निजामुद्दीन औलिया जैसे श्रद्धेय तीर्थस्थलों से जुड़े हैं.
हालाँकि, जबकि सूफीवाद आत्मा का पोषण करता है, यह अक्सर व्यापक सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने में कम पड़ जाता है.इसके अलावा, कुछ तिमाहियों में, सूफी प्रथाओं का व्यवसायीकरण हो गया है, जहाँ प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों का आदान-प्रदान पैसे के लिए किया जाता है.
यह जीवन के लिए एक व्यापक मार्गदर्शक के रूप में सूफीवाद की भूमिका को कमज़ोर करता है. दूसरी ओर, भारतीय मुसलमानों का तर्कवादी वर्ग, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द जैसे धर्मनिरपेक्ष संस्थानों में शिक्षित हैं, आस्था को बौद्धिकता के साथ जोड़ते हैं.
वे इस्लामी शिक्षाओं को समकालीन दुनिया के ज्ञान के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे एक ऐसा समुदाय बनाने की उम्मीद होती है जो आधुनिकता को अपनाते हुए इस्लामी मूल्यों को बनाए रखता है.
फिर भी, अपनी प्रासंगिकता के बावजूद, तर्कवादियों को उलेमा से काफी विरोध का सामना करना पड़ता है, जो अक्सर आधुनिक शिक्षा को धार्मिक विश्वास के साथ असंगत मानते हैं.
इस विरोध ने कई तर्कवादियों को अपने बौद्धिक हलकों में वापस जाने के लिए प्रेरित किया है, जो प्रतिक्रिया के डर से व्यापक समाज के साथ जुड़ने में झिझकते हैं. वर्तमान में, उलेमा, सूफीवाद और तर्कवाद अलग-अलग हिस्सों में बंटे हुए हैं, जो सार्थक रूप से एक दूसरे से जुड़ने में असमर्थ हैं. यह विभाजन आज मुस्लिम समुदाय की प्रगति में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक हैं.
ऐसे मंच बनाने की तत्काल आवश्यकता है जहाँ ये विचारधाराएँ एक-दूसरे से जुड़ सकें, अपने मतभेदों पर चर्चा कर सकें और आम समाधानों की दिशा में काम कर सकें.
ऐतिहासिक रूप से, वहाबीवाद जैसे आंदोलनों का उदय और ISIS जैसे चरमपंथी समूहों के प्रभाव ने इस्लामी विचारों में असंतुलन के खतरों को उजागर किया है.
उदाहरण के लिए, 11वीं शताब्दी में मुताज़िला तर्कवादियों के चरम रुख ने धार्मिक मतभेद पैदा कर दिया, जिसे इमाम ग़ज़ाली जैसे विद्वानों ने संबोधित किया, जिन्होंने इस्लाम की पारंपरिक व्याख्याओं को फिर से स्थापित करने की कोशिश की.
ओटोमन्स द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को अस्वीकार करने से बौद्धिक प्रगति में और बाधा उत्पन्न हुई, क्योंकि इसने नए विचारों के प्रसार को सीमित कर दिया. 20वीं शताब्दी में भी, उपनिवेशवाद के सामने आधुनिकता के प्रतिरोध ने अल्लामा इकबाल जैसे लोगों को दक्षिण एशिया में मुसलमानों के लिए एक नई मेटा-कथा पेश करने के लिए प्रेरित किया, जो धार्मिक सिद्धांतों से समझौता किए बिना एकता और प्रगति की मांग कर रही थी.
भारतीय मुस्लिम पहचान का एक महत्वपूर्ण पहलू हिंदू धर्म से इसका संबंध है. भारतीय मुसलमान अपनी सांस्कृतिक विरासत को अस्वीकार करने का जोखिम नहीं उठा सकते, जिसे हिंदू धर्म के साथ सदियों के संपर्क ने आकार दिया है. विशेष रूप से इस्लामी पहचान के पक्ष में इस संबंध को तोड़ने का कोई भी प्रयास उन्हें केवल बड़े समाज से अलग कर देगा और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाएगा.
साझा सांस्कृतिक इतिहास को स्वीकार करने के लिए इस्लामी सिद्धांतों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है. बल्कि, यह मुसलमानों को समृद्ध बौद्धिक और सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाने की अनुमति देता है, जिसने उनके जीवन के तरीके को प्रभावित किया है - भोजन और कपड़ों से लेकर वास्तुकला तक.
आज, दुनिया भर के मुस्लिम विद्वान भी, जिनमें पाकिस्तान के विद्वान भी शामिल हैं, भगवद गीता, वेद और उपनिषद जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों का पुनरावलोकन कर रहे हैं. भारतीय मुसलमानों को भी ऐसा ही करना चाहिए, अपने विश्वास को कम करने के लिए नहीं, बल्कि दोनों समुदायों के बीच आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देने के लिए.
इस्लामी और हिंदू दोनों बौद्धिक परंपराओं से जुड़कर, भारतीय मुसलमान अपने ज्ञान को समृद्ध कर सकते हैं और एक अधिक शांतिपूर्ण, प्रगतिशील समाज में योगदान दे सकते हैं.
ऐसा दृष्टिकोण संवाद, सहयोग और अंततः पूरे देश के लिए सामूहिक प्रगति को बढ़ावा देगा. इस ईद पर, मजीद खुतबा (उपदेश) न केवल मुसलमानों की सुरक्षा के लिए प्रार्थनाओं पर केंद्रित हों, बल्कि समुदाय के भीतर विभाजन को पाटने वाले एक नए मेटा-कथा के निर्माण का आह्वान भी करें.
उलेमा, सूफियों और तर्कवादियों के बीच पुल बनाना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है, और यह प्रयास करने लायक कार्य है. केवल सहयोग के माध्यम से ही मुसलमान तेजी से बदलती दुनिया में अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकते हैं.
(लेखक आवाज द वाॅयस के प्रधान संपादक हैं)
.webp)