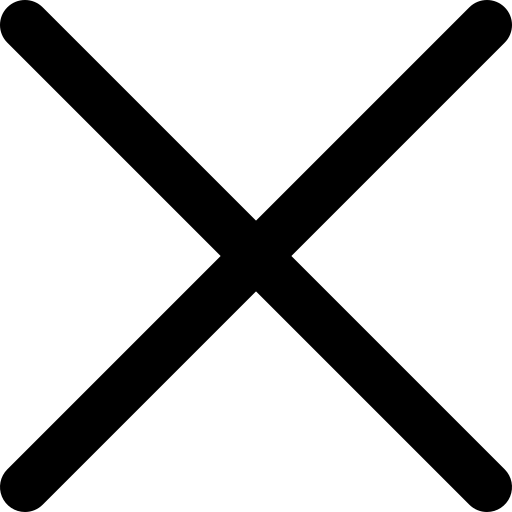.webp)
 साकिब सलीम
साकिब सलीम
अहमत टी. कुरु ने अपनी विचारोत्तेजक पुस्तक, इस्लाम, अधिनायकवाद और अविकसितता की शुरुआत में सवाल उठाया है, “मुस्लिम-बहुल देश कम शांतिपूर्ण, कम लोकतांत्रिक, कम विकसित क्यों हैं?” इसका उत्तर पाने के लिए कुरु ने इस घटना के दो सबसे प्रचलित स्पष्टीकरणों का सहारा लिया.
1.) “कई विश्लेषकों ने विभिन्न मुस्लिम समाजों में हिंसा के उदय के लिए पश्चिमी उपनिवेशवाद को दोषी ठहराया है.”
2.) “कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि - इसके ग्रंथों या इतिहास के आधार पर - इस्लाम में कुछ आवश्यक विशेषताएं हैं जो हिंसा से जुड़ी हैं.”
कुरु ने दोनों स्पष्टीकरणों को खारिज कर दिया और उलेमा-राज्य गठबंधन को दोषी ठहराया, जो उनके अनुसार, ग्यारहवीं शताब्दी के आसपास विकसित हुआ था और बौद्धिक स्वतंत्रता को कमजोर करने के साथ-साथ बुर्जुआ वर्ग के उदय को भी रोका था. उनका तर्क है, "उपनिवेशवाद विरोधी दृष्टिकोण दुनिया के अन्य भागों के प्रति पश्चिमी देशों की नीतियों के प्रभाव पर अत्यधिक जोर देता है
, जबकि गैर-पश्चिमी देशों की अपनी घरेलू और क्षेत्रीय गतिशीलता की भूमिका को कम करके आंकता है. इसलिए, यह स्पष्ट नहीं कर सकता कि मुसलमानों ने पश्चिमी औपनिवेशिक शक्तियों और कब्ज़ेदारों के खिलाफ़ लड़ने के बजाय अन्य मुसलमानों द्वारा और उनके खिलाफ़ अंतरराज्यीय युद्ध, गृह युद्ध और आतंकवाद का सामना क्यों किया है."
इस्लाम के मामले में, कुरु बताते हैं कि इस्लामी शासन की पहली तीन शताब्दियों के दौरान बुद्धिजीवियों का उदय और व्यापारिक वर्ग का विकास यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि धर्म स्वाभाविक रूप से 'हिंसक' या 'प्रतिगामी' नहीं है.
लेखक, हालांकि, घोषणा करते हैं, "यह मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, इतिहास की नहीं. यह समकालीन समस्याओं का विश्लेषण करती है और उनकी उत्पत्ति को समझने के लिए इतिहास की खोज करती है." लेकिन ऐतिहासिक ग्रंथों और संदर्भों का उनका विश्लेषण इतिहास के किसी भी छात्र के लिए रुचि पैदा कर सकता है.
मेरे लिए दिलचस्प बात यह थी कि कुरु का तर्क था कि शुरुआती इस्लामी विद्वान, उलेमा, खुद को राजनीतिक नियंत्रण से अछूता रखने के लिए राज्य या शासक अभिजात वर्ग से खुद को दूर रखते थे. इसके बजाय, उन्हें या तो व्यापारियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता था या वे खुद ही अपने शैक्षणिक कार्यों के लिए व्यापार करते थे.
वह इस बात को स्पष्ट करने के लिए डेटा और उदाहरण प्रदान करता है. वहाँ से, वह तर्क देता है कि ग्यारहवीं शताब्दी के दौरान ग़ज़ाली जैसे विद्वानों ने एक सिद्धांत का बीड़ा उठाया कि धर्म और राज्य अविभाज्य हैं. लेखक के अनुसार, धर्म और राज्य के अन्योन्याश्रित होने का विचार इस्लामी विद्वानों पर फ़ारसी प्रभाव था.
और, यह विचार मुसलमानों के बीच आम मुस्लिम प्रवचन पर हावी है और इस दृष्टिकोण से असहमत होने वाले किसी भी विद्वान को हाशिए पर डाल दिया जाता है. यह तर्क कि एक स्वतंत्र मजबूत व्यापारी वर्ग बुद्धिजीवियों का समर्थन करता है और 11वीं शताब्दी से मुस्लिम समाजों में इस वर्ग की कमी ने मुस्लिम समाजों में वैज्ञानिक विकास में समग्र गिरावट की ओर अग्रसर किया है, बहुत कुछ समझाता है लेकिन अभी भी अधिक ऐतिहासिक जांच का अभाव है.
ब्रुक एडम्स, विक्टोरिया मिरोशनिक, दीपक बसु आदि कई विद्वानों ने बताया है कि औद्योगिक क्रांति, जिसने हमारे विश्व को हमेशा के लिए बदल दिया, वास्तव में 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा बंगाल से लूटे गए धन से प्रेरित थी. इस समय के आसपास इंग्लैंड में विशेष रूप से कपड़ा उद्योग को मशीनीकृत करने के लिए कई आविष्कार और खोजें की गईं.
यह तर्क कुरु के इस दावे को पुष्ट करता है कि एक स्वतंत्र व्यापारी वर्ग वास्तव में बौद्धिक और वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देता है.लेकिन, कुरु दो महत्वपूर्ण घटनाओं से नहीं जुड़ते हैं. मुगलों के अधीन भारतीय समाज, जिन्होंने 16वीं और 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत पर शासन किया, ने व्यापारी जातियों को उच्च सम्मान दिया.
व्यापारी काफी हद तक राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र थे और दूर-दूर के देशों के साथ व्यापार करते थे. भारतीय जाति व्यवस्था का प्रभाव, जिसने व्यापारियों को तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक समूह माना, ने यह भी सुनिश्चित किया कि व्यापारियों को एक निश्चित हद तक स्वायत्तता प्राप्त हो. यह उस समय भारत के समग्र बौद्धिक विकास में नहीं बदला, जो उसी अवधि के आसपास यूरोप के उदय की बराबरी कर सकता था.
ऐतिहासिक रूप से, प्राचीन भारत और प्राचीन ग्रीस में राज्य प्रायोजित विद्वानों ने अपने समय के बौद्धिक विकास का नेतृत्व किया था. हमारे समय में, राज्य नियंत्रित विश्वविद्यालयों, विशेष रूप से यूएसएसआर में, ने हमें कई सफल वैज्ञानिक विकास प्रदान किए थे. 20वीं शताब्दी के बाद के विश्व युद्ध के दौरान बौद्धिक विकास में पश्चिमी यूरोप से प्रतिस्पर्धा करने वाले समाजवादी और साम्यवादी देशों में कोई स्वतंत्र व्यापारी वर्ग नहीं था.
कुरू यह भी तर्क देते हैं कि मुस्लिम देशों में धर्मनिरपेक्ष और इस्लामवादी दोनों तरह के अधिनायकवादी शासन को विकसित करने की अधिक प्रवृत्ति है. अविकसितता और वैज्ञानिक विकास की कमी के साथ अधिनायकवाद के संबंध पर अधिक बहस होनी चाहिए थी. पाठकों को यह समझने की आवश्यकता है कि चीनी या सोवियत अधिनायकवाद ने उन समाजों में ऐसे विकास में बाधा नहीं डाली.
लेखक ने यह बताकर सही बात कही है कि ‘किराए पर लेने की प्रथा’ ने “अधिकांश मुस्लिम देशों में गैर-उत्पादक राजनीतिक और धार्मिक अभिजात वर्ग के प्रभुत्व को बढ़ाने में मदद की है. इन किराए ने कई इस्लामवादी शासनों को जीवित रहने में सक्षम बनाया है, जिन पर उलेमा (जैसे ईरान) या उलेमा-राजशाही गठबंधन (जैसे सऊदी अरब) का प्रभुत्व है.
कुछ अन्य मुस्लिम मामलों में, तेल राजस्व की अनुपस्थिति ने राजनीतिक अधिकारियों को अर्थव्यवस्था और समाज पर राज्य के नियंत्रण को कम करने के लिए मजबूर किया. लेकिन इन राजनेताओं ने आम तौर पर किराए की तलाश जारी रखी है.
राज्यवादी सामाजिक-आर्थिक नीतियों पर वापस जाने के तरीके खोजे. तर्क यह है कि इन किराएदार राज्यों की सरकारें लोगों के करों पर निर्भर नहीं हैं . इस प्रकार वे अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए ऐसे तरीके से काम करती हैं जिन्हें प्रतिगामी या स्थिर कहा जा सकता है.
एक भारतीय पाठक के रूप में, यह मेरे लिए अधिक दिलचस्प होता अगर लेखक भारतीय मुस्लिम समाज से भी जुड़ते. तथ्य यह है कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और 1947 तक सबसे बड़ी आबादी हुआ करती थी (अब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच विभाजित है) इसे एक केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत करता है.
तब्लीगी जमात, देवबंद स्कूल आदि जैसे भारतीय मुस्लिम संगठन एक बड़ी वैश्विक आबादी को आकर्षित करते हैं. कोई यह देखना पसंद करेगा कि कुरु ने भारतीय उलेमा (विशेषकर देवबंद स्कूल) के साथ कैसे बातचीत की होगी, जिन्होंने महात्मा गांधी (एक हिंदू) को अपना नेता स्वीकार किया था.
दिलचस्प बात यह है कि भारत के मामले में, यह 'धर्मनिरपेक्ष' शिक्षित मोहम्मद अली जिन्ना थे जो एक धार्मिक राज्य चाहते थे, जबकि जमीयत-ए-उलमा (इस्लामिक विद्वानों का संघ) ने कथित रूप से एक 'हिंदू पार्टी', कांग्रेस के नेतृत्व में एक धर्मनिरपेक्ष भारत के समर्थन में तर्क दिया था.
पुस्तक पढ़ने के लिए सम्मोहक है. यह अच्छी तरह से शोध की गई पुस्तक शोधकर्ताओं को और अधिक सवाल पूछने के लिए प्रेरित करेगी. इसमें जांच के नए द्वार खोलने की सभी क्षमताएं हैं. लेखक कठिन सवाल उठाता है, जवाब देने की कोशिश करता है और इससे भी ज्यादा अपने पाठकों को रुकने और सोचने के लिए मजबूर करता है. वह इस विषय पर मौजूदा विद्वता पर सवाल उठाता है और आगे के शोध के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करता है.